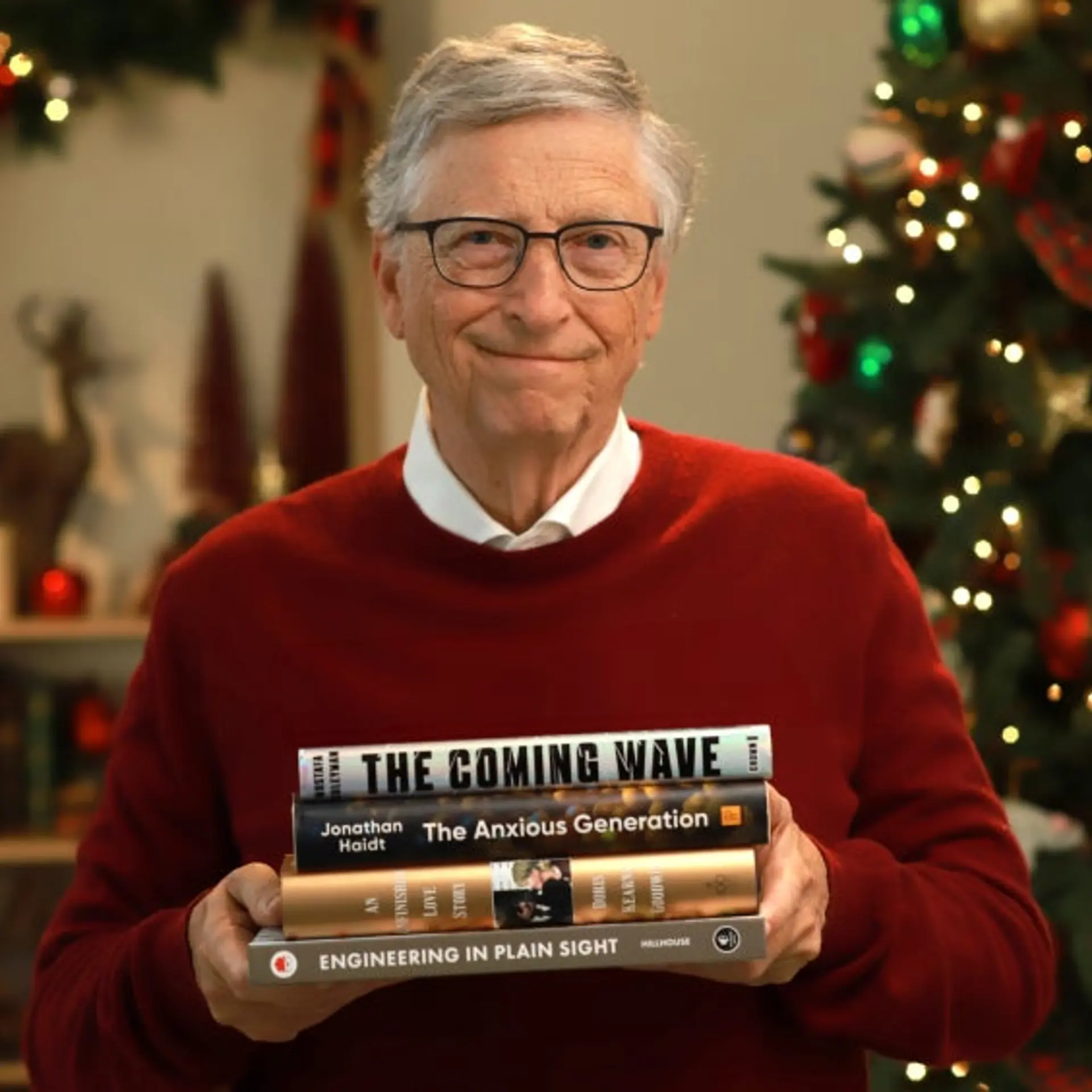भारत की यातायात समस्याओं से निबटने का एक विकल्प प्रदान करतीं हाई-वेलोसिटी सड़कें
इस लेख मेें हम आपको श्रमण मित्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक ‘विज़न इंडिया 2020 (Vision India 2020) के कुछ अध्यायों को साझा कर रहे हैं जिनमें स्टार्टअप कंपनियों के लिये अपने उद्यम को अरबों डाॅलर के उद्यमों में बदलने के 45 दिलचस्प विचारों की रूपरेखा रखी गई है। यह सभी लेख व्यापार फिक्शन के रूप में यह मानते हुए लिखे गए हैं कि हम 2020 में रह रहे हैं जिनमें यह दर्शाया गया है कि कैसे ये व्यापार बीते एक दशक में स्थापित किये गए हैं। हमें उम्मीद है कि ये लेख आपके भीतर अपना एक सफल स्टार्टअप प्रारंभ करने के लिये चल रहे विचारों को नया आयाम देने में सफल होगा।

भारतीय उद्योग परिसंघ और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का अनुमान है कि भारत में विनिर्माण का क्षेत्र वर्ष 2007 के 272 बिलियन डाॅलर के मुकाबले वर्ष 2014 में 520 बिलियन डाॅलर के बाजार पूंजीकरण को पाने में सफल रहेगा। भारत को अपने उपभोक्ताओं की तेजी से बढ़ती कारों से लेकर उपकरणों, कंप्यूटरों से लेकर मोबाइल फोनों, माॅड्यूलों से लेकर घटकों की मांग को पूरा करने के लिये लगातार निर्माण करने रहने की आवश्यकता है। हालांकि वर्ष 2009 में भारत की सड़क व्यवस्था शहर से विभिन्न उत्पादों को शहर और बंदरगाह से बंदरगाह तक उच्च गति से ले जाने के काबिल नहीं है।
हालांकि सड़क परिवहन मंत्रालय लगातार राष्ट्रीय राजमार्गों के जीर्णोद्धार के काम में बड़े पैमाने पर प्रगति करता दिख रहा है लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच जुड़ाव या इंटरकनेक्टिविटी अभी भी आदर्श के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा विभिन्न कारखानों की ओर आने वाले कच्चे माल और तैयार उत्पाद को ले जाने वाली क्षेत्रीय सड़कों की हालत तो और भी शोचनीय है। मुझे याद नहीं है कि ऐसा मेरे साथ कितनी बार हुआ है जब मैं सड़कों पर मीलों तक गाडि़यों के लगे ट्रेफिक जाम में फंसा रहा हूँ। ‘‘पुल टूट गया है,’’ ड्राईवर रियरव्यू मिरर में मुझे देखते हुए कहता है। ‘‘दोबारा’’
इसके जवाब में हमने विनिर्माण के क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आठ लेन वाली एक टोल रोड की परियोजना तैयार की है जो सरकारी नौकरशाही के बजाय पेशेवर प्रबंधकों की निगरानी में तैयार होगी और इसकी देखरेख भी इनके ही जिम्मे होगी। यह सड़क देश और दुनिया की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति को पूरा करने के लिये लगातार दौड़ रही गाडि़यों के लिये कारगर रहने की उम्मीद है।
भारत में सिर्फ कोयले की आवाजाही ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र है क्योंकि कोयला पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी महाराष्ट्र भर में फैला हुआ है। इन प्रदेशों में कोयले के अलावा आर्सेलर मित्तल, टाटा स्टील, एस्सार, जिंदल और कई अन्य इस्पात संयत्र भी फलफूल रहे हैं। इसके अलावा अब झारखंड के एक हिस्से जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के सबसे बड़े निर्माण कारखानों में से एक स्थित है। अगर हम इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी महाराष्ट्र के सीमेंट संयंत्रों को भी जोड़ दें तो हमें औद्योगिक क्षताओं से भरपूर परिवहन प्रणाली के बहुत सख्त आवश्यकता है।
इस सात राज्यों के मध्य यातायात के प्रवाह पर ध्याान केंद्रित करते हुए और कोयले, स्टील, सीमेंट और आॅटो जैसे उद्योगों को नजर में रखते हुए हम अपने आधार को मान्य करने के लिये निकल पड़े। सबसे पहले हमने इस क्षेत्र में कारोबार करने वाली प्रत्येक प्रमुख कंपनी के साथ बैठक की और उनकी परिवहन से संबंधित मार्गों और आवश्यकताओं को चिन्हित किया। इन दौरान इनके सामने कुछ परेशानी पैदा करने वाले हालात भी आए। यह प्रारंभ से ही स्पष्ट था कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हल्दिया, उड़ीसा के पारद्वीप और आंध्र के विज़ाग के बंदरगाहों के अलावा अंदरूनी मार्गों पर भी अच्छी कनेक्टिविटी की आवश्यकता है।
हमारी योजना बहुत तेजी से आगे बढ़ी और हमने वर्ष 2010 से 2015 के मध्य भारत के निर्माण के क्षेत्र के प्रमुख केंद्रों को आपस में जोड़ने वाले इलाकों को इंटरकनेक्ट करने वाले क्षेत्रों में करीब 1 हजार किलोमीटर का नेटवर्क तैयार किया। जमशेदपुर और कोलकाता पोर्ट के बीच कनेक्टिविटी के लिये सीधा संपर्क समय की मांग थी। टाट स्टील प्रतिमाह जापानी कार निर्माता कंपनी को 30 से 60 टन के बीच शीट मेटल की पूर्ती करती थी। लेकिन प्रतिमाह ऐसा होता था कि 8 से 10 ट्रक रास्ते में कहीं फंस जाते थे जिसके चलते जहाज की लोडिंग में देरी होती थी। बीते कई दशकों से हमारे देश की सड़कों पर चलने वाले गतिरोध के आदी हो चुके हैं और ऐसे में जब ड्राईवरों को साफसुथरी और सीधी सड़कें मिलने लगीं तो उन्होंने भी उनका आनंद उठाना प्रारंभ कर दिया।
हमनें राउरकेला के स्टील संयंत्रों को उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा। हमनें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 के किनारे पर स्थित कारखानों को हल्दिया बंदरगाह से जोड़ा। हमनें झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 और 33 को कई बिंदुओं पर आपस में जोड़ा जिससे खनिजों का प्रवाह बहुत आसान हो गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हमने जादूई कालीन बनाने वालों के लिये एनएच 43 के आसपास के क्षेत्र पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया।
यह कहने की जरूरत ही नहीं है कि इस अविश्वसनीय रूप से इतनी महंगी परियोजना को वित्तीय इंजीनियरिंग बनाना एक महत्वपूर्ण कारक रहा। परिवहन मंत्रालय ने अपनी आर्थिक महत्व की परियोजनाओं नामक योजना के तहत हमें 50 प्रतिशत ऋण वित्तपोषण की पेशकश की। ऋण के फलस्वरूप परियोजना पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिये इसपर 20 वर्षों की रोक लगा दी गई थी। साथ ही बिल्कुल समान शर्तों के तहत एशियन डवलपमेंट बैंक ने भी 25 प्रतिशत निवेश किया। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारों ने भी 5 प्रतिशत का सहयोग किया। और बचा हुआ अंतिम 20 प्रतिशत टेक्सास पैसिफिक समूह और केकेआर के माध्यम से इक्विटी फाइनेंसिंग के माध्यम से संभव हुआ। इस परियोजना की कुल लागत 10 बिलियन डाॅलर है जो इसके निरंतर बढ़ते हुए चरणों के साथ पांच बार में मिलेगा।
वर्ष 2015 आते-आते मैजिक कारपेट आठ लेन वाली टोल सड़कों का एक पूरा नेटवर्क तैयार कर चुका था जिसमें प्रत्येक टोल प्लाजा पर परिचालन को बेरोकटोक संचालित करने के लिये 32 टोल गेट तैयार किये गए हैं। प्रत्येक प्लाजा पर भुगतान करने के तीन विकल्प मौजूद हैं जिनमें मानव टोल कलेक्टर नकछ या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से टोल वसूलते हैं। इसके अलावा संपर्करहित प्रीपेड कार्डों को कलेक्टर के हवाले करने के विकल्प के अलावा स्वचालित रूप से संचालित होने वाले ट्रांसपोंडर की भी सुविधा उपलब्ध है।
इस नेटवर्क ने न सिर्फ भारतभर में माल की आवाजाही पर ही एक बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ा है बल्कि इसके फलस्वरूप कोलकाता, जमशेदपुर, रांची, खड़गपुर, भुवनेश्वर और इनसे भी बहुत आगे शहरी भीड़भाड़ से छुटकारा मिला है। एक बार इन शहरों के उन मुख्य इलाकों से मालवाहक वाहनों को दूर करने के बाद मैजिक कारपेट ने इन रास्तों पर इंसानी आवाजाही के लिये जगह बना दी। हमारे क्षेत्र में यात्रा के दौरान आवाजाही में लगने वाले समय में एक तिहाई की कमी देखने को मिल रही है। कभी घंटों में निबटने वाली यात्रा अब मात्र 15 से 20 मिनट में ही समाप्त हो जाती है और 6 घंटे की यात्राएं तो केवल दो घंटे ही लेती हैं।


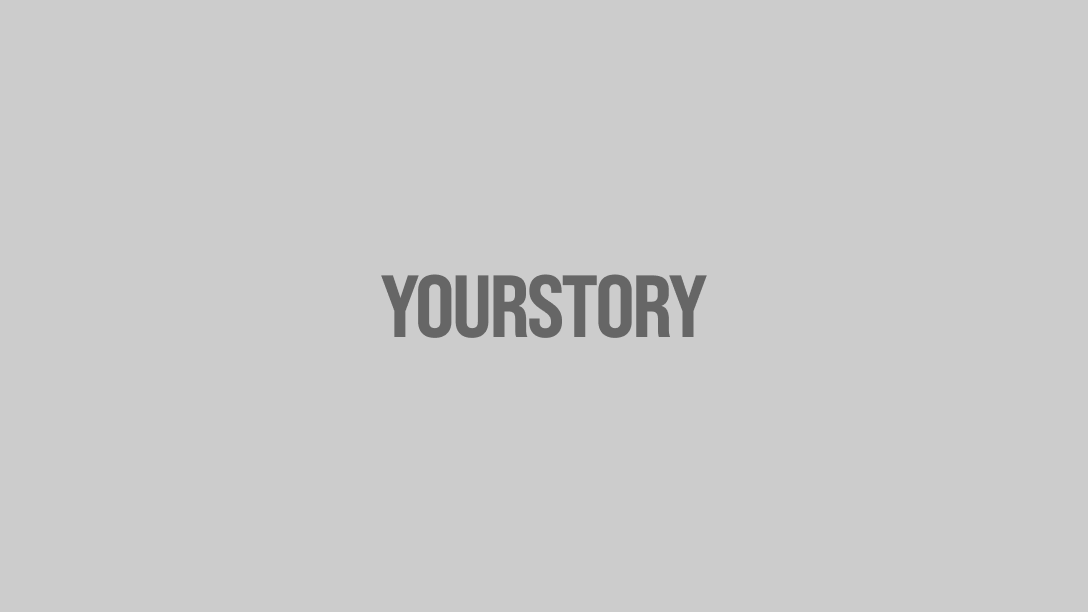


![[फंडिंग अलर्ट] होम डिजाइन स्टार्टअप लिवस्पेस ने जुटाया 90 मिलियन डॉलर का निवेश](https://images.yourstory.com/cs/12/511c01b01fd011ea8217c582b4ed63bb/Imagebsgz-15991116935511-1599148196686.jpg?mode=crop&crop=faces&ar=1%3A1&format=auto&w=1920&q=75)