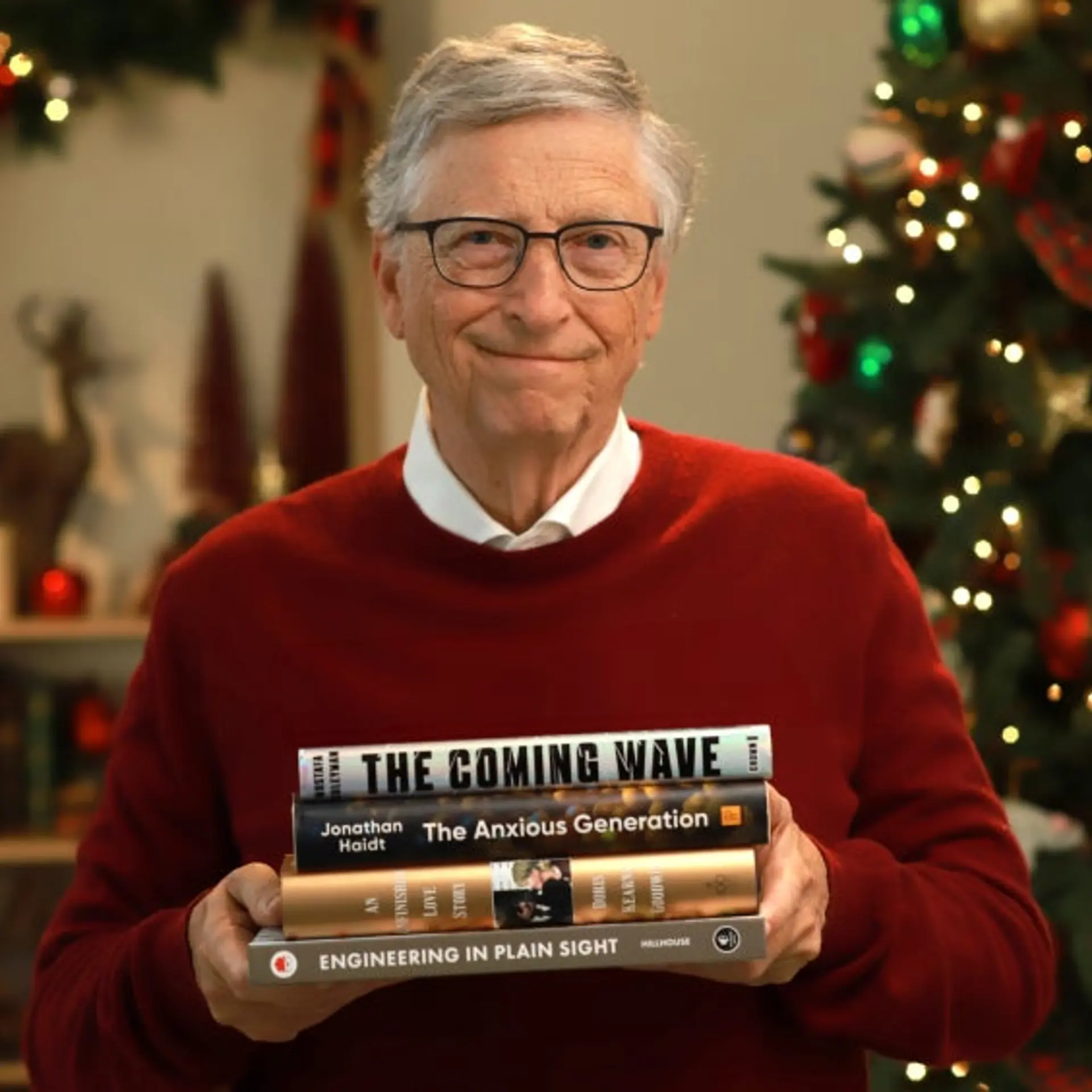विज्ञान पढ़ तो रही हैं महिलाएं, लेकिन उनके वैज्ञानिक बनने की राह अब भी आसान नहीं
महिलाएं विज्ञान पढ़ तो रही हैं, लेकिन जितनी विज्ञान पढ़ रही हैं, उतनी वैज्ञानिक नहीं बन रहीं. जो वैज्ञानिक बन भी रही हैं, वो भी बड़े जिम्मेदारों पदों से अभी काफी दूर हैं. महिलाओं के लिए क्यों इतनी कठिन है वैज्ञानिक होने की राह.
90 साल पहले भारत की पहली महिला वैज्ञानिक कमला सोहनी को इस देश के सबसे प्रतिष्ठित साइंस इंस्टीट्यूट ने अपने यहां दाखिला देने से यह कहकर इनकार कर दिया था कि महिलाओं में विज्ञान पढ़ने की बुद्धि नहीं होती. तब से लेकर अब तक दुनिया और देश, दोनों काफी बदल चुके हैं. पिछले दो दशकों का ग्राफ कहता है कि विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. हालांकि ग्रेजुएशन से लेकर डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च तक में महिलाओं की संख्या बढ़ने और कई बार पुरुषों से ज्यादा होने के बावजूद महत्वपूर्ण और फैसलाकुन पदों पर बैठे वैज्ञानिकों के जेंडर अनुपात में बेहतरी का ग्राफ उतनी तेजी से नहीं बदला है.
महिलाएं विज्ञान पढ़ तो रही हैं, लेकिन जितनी विज्ञान पढ़ रही हैं, उतनी वैज्ञानिक नहीं बन रहीं. जो वैज्ञानिक बन भी रही हैं, वो भी बड़े जिम्मेदारों पदों से अभी काफी दूर हैं. संस्थाओं की कमान अब भी उनके हाथों में नहीं है.
भारत में स्टेम यानि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमैटिक्स में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की दो महिलाओं ने 130 महिला वैज्ञानिकों का इंटरव्यू किया. अनिता कुरुप एनआईएएस में एजूकेशन फॉर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड प्रोग्राम की हेड हैं और अंजलि राज स्टेम प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट हैं. इन दोनों महिलाओं का यह जॉइंट रिसर्च पेपर सेज के साइंस जरनल में प्रकाशित हुआ है.
लगभग 7000 शब्दों का यह लंबा रिसर्च पेपर इस बात पड़ताल की कोशिश है कि भारत में स्टेम के क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति हैं और उसकी वजह क्या है. साइंटिफिक रिसर्च का काम 9 से 6 की नौकरी नहीं है. यह लंबे और गहरे श्रम की मांग करता है. इस क्षेत्र में परिश्रम बहुत ज्यादा और पैसा उसकी तुलना में कम है. विज्ञान में गहरी रुचि और अपने काम के लिए जुनून ही आपको विज्ञान के क्षेत्र में लंबे समय तक टिकाए रख सकता है.
यह रिसर्च कहती है कि वैज्ञानिक शोध और रिसर्च के क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित करने के बावजूद वैज्ञानिक संस्थाओं और भारतीय परिवारों का सामंती और मर्दवादी ढांचा अब भी महिलाओं को वह सपोर्ट सिस्टम नहीं दे पा रहा, जिसकी उन्हें जरूरत है. केयरगिविंग आज भी मुख्य रूप से महिलाओं का ही इलाका है. घर-परिवार की जिम्मेदारियां मुख्य रूप से औरतों के कंधों पर ही हैं. इन जिम्मेदारियों के साथ नौकरी तो की जा सकती है, लेकिन साइंस रिसर्च नहीं हो सकती.
आज हम अगर किसी से भी जेंडर भेदभाव की बात करें तो उनका जवाब यही होता है कि अब समय बदल गया है. अब कहीं कोई जेंडर भेदभाव नहीं है. यह स्टडी कहती है कि यह हमारे समय का सबसे बड़ा पूर्वाग्रह है कि अब कोई पूर्वाग्रह नहीं रहे. अनिता कुरुप कहती हैं कि पुरुष वैज्ञानिकों के सामने काम और परिवार के बीच संतुलन बिठाने जैसा कोई सवाल ही नहीं होता. लेकिन हमने जितनी भी महिला वैज्ञानिकों से बात की, उन सबकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि वो अपनी रिसर्च और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे कायम करें.
अनिता कुरुप और अंजलि राज ने 2016 से 2018 तक 130 महिला वैज्ञानिकों के लंबे इंटरव्यू किए. इस इंटरव्यू की फाइंडिंग्स डेटा पर ज्यादा जोर देने के बजाय लंबे पर्सनल नरेटिव में बात करती है. महिला वैज्ञानिकों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. उनके परिवार और पार्टनर्स कितने सपोर्टिव हैं. बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाता है, प्राइमरी केयरगिविंग किसके हिस्से में आती है. रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्ट्रक्चर महिलाओं के प्रति कितना संवेदनशील और जिम्मेदार है. प्रयोगशाला में उन्हें किस तरह के पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है. बहुत सारी महिलाओं को जिम्मेदारियों के कारण अपनी प्रोफेशनल महत्वाकांक्षाओं को मुल्तवी करना पड़ता है और कई बार रिसर्च को महत्व देने वाली महिलाओं को निजी मोर्चे पर बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं.
यह रिसर्च इस ओर इशारा करती है कि वर्कप्लेस पर महिला कर्मियों के लिए जिन बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए कानून भी बना हुआ है, उन कानूनों का भी अधिकांश जगहों पर पालन नहीं किया जा रहा. जैसे मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट, 2017 के मुताबिक जिस भी जगह पर 50 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, वहां क्रैच होना अनिवार्य है. लेकिन आज की तारीख में अधिकांश साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ये बुनियादी सुविधा भी नहीं है.
इस रिसर्च पेपर को आप विस्तार से यहां पढ़ सकते हैं. पढि़ए और विचार करिए कि सबके लिए न्याय और बराबरी की बात करने वाले देश में बहुत बुनियादी जेंडर बराबरी अभी भी बहुत दूर की कौड़ी है. हम वहां से तो आगे आ गए हैं, जहां कमला सोहनी को सिर्फ विज्ञान पढ़ने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी थी, लेकिन उस जगह पहुंचने में अभी बहुत लंबा सफर तय करना बाकी है, जहां वो पुरुषों की तरह बड़ी वैज्ञानिक, बड़ी खोजकर्ता हो सकें. विज्ञान के लिए जीवन लुटा सकें. विज्ञान पढ़ने वाली बहुत सारी महिलाएं विज्ञान पढ़कर हाउस वाइफ न बन जाएं, बल्कि सचमुच वैज्ञानिक बन सकें.