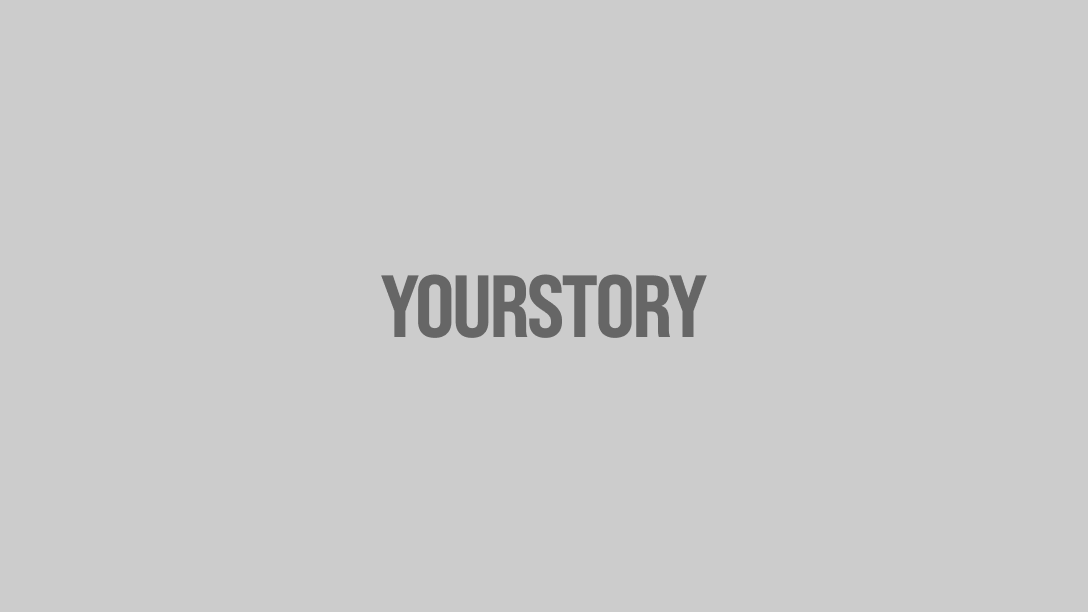बचपन में घर के चूल्हे की आग से निकलती रोशनी में पढ़ाई करने वाले मूर्ति अब सर्जिकल लाइट में बच्चों की बीमारियों को कर रहे हैं दूर
मूर्ति का जन्म एक ग़रीब किसान परिवार में हुआ ... बेटे की पढ़ाई में कोई तक़लीफ़ न आये इस लिए माता-पिता ने दूसरों के यहाँ भी की मज़दूरी ... मूर्ति ने भी माँ-बाप की मदद के लिए खेतों में किया काम ... कंदील की रोशनी में की पढ़ाई ... चूल्हा जलने पर कंदील बुझा देते और चूल्हे की रोशनी में करते पढ़ाई ताकि कंदील का तेल बच सके ... ग्रामीण परिवेश से होने की वज़ह से अंग्रेज़ी को अडॉप्ट करने में आयी तक़लीफ़ें ... एमबीबीएस कोर्स के पहले साल में ही मोटे और भारी-भरकम शब्दों से इतना घबरा गए कि गाँव लौट आये ... पिता ने जब जिम्मेदारियों का अहसास दिलाया तो लौटे मेडिकल कॉलेज ... पढ़ाई पूरी की, डॉक्टर बने और दूर की घर-परिवार की ग़रीबी ... ईएनटी सर्जन बनकर ख़ूब नाम कमाया ... कान, नाक और गले से जुड़ी बच्चों की बीमारियों को दूर करने में हासिल कर चुके हैं महारत
एक गाँव है, उसमें एक किसान का घर है। जैसा कि हर छोटे और ग़रीब किसान का घर होता है वैसा ही उस किसान का भी घर है। पत्थरों के ऊबड़-खाबड़ टुकड़ों से बनी दीवारें हैं और मिट्टी से बनी और सनी छत। न बिजली है, न पानी का नल। घर में मिट्टी का ही चूल्हा है। छोटे से इस घर में पूरा परिवार रहता है। किसान, उसकी पत्नी, चार बच्चे - एक लड़का और तीन लडकियां। सभी इसी घर में रहते हैं। किसान की आमदनी का ज़रिया भी एक ही है - खेत। खेत में अच्छी फ़सल हुई तो आमदनी, नहीं तो दूसरों के यहाँ मज़दूरी करने की मज़बूरी। चूँकि किसान ग़रीब है और अकेले छह लोगों का पेट भर नहीं सकता, खेती के काम में सभी उसकी मदद करते हैं। बच्चे भी अपने नन्हें हाथों से जो कर पाते हैं वो करते हैं। एक दिन किसान को अहसास होता है कि अगर उसका बच्चा भी उसी की तरह अनपढ़ रहा तो वो भी ग़रीब ही रहेगा और परेशानियाँ उसे घेरे रहेंगी। किसान एक बड़ा फ़ैसला करता है। वो अपने बच्चे को स्कूल भेजता है । बच्चा स्कूल में अच्छे से पढ़े इसके लिए वो अपनी पत्नी के साथ दिन-रात मेहनत करता है। अपने खेत में तो काम करता ही है, आमदनी कुछ ज्यादा हो जाय और बच्चे की स्कूल की ज़रूरतें पूरी हो जायँ, इस मक़सद से दूसरों के यहाँ मज़दूरी भी करता है। माँ-बाप की तक़लीफ़ों को देखकर बच्चा पढ़ाई में जी-जान लगा देता है। घर में बिजली नहीं है तब भी रात के अँधेरे में भी बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकती। बच्चा कंदील की रोशनी में पढ़ता है। और तो और, जब माँ चूल्हे पर खाना बना रही होती है तब बच्चा लकड़ियों के जलने पर निकलने वाली आग की रोशनी में पढ़ाई करता है, ताकि कंदील का तेल बच सके। यही बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बनता है। मशहूर सर्जन हो जाता है। समाज में उसका ख़ूब नाम होता। दुनिया उसको सलाम करती है।
ये पढ़कर आपको शायद लगेगा कि ये किसी फ़िल्मी कहानी का हिस्सा है। शायद लगे कि किसी टीवी सीरियल की कहानी का सारांश। किसी को शायद ये भी लगे कि किसी रचनाकार की कल्पना है, किसी कल्पित कहानी का एक हिस्सा। लेकिन ये बातें न फ़िल्मी है न कल्पना। ये हक़ीक़त में एक शख्शियत की ज़िंदगी की कहानी है। कहानी रोचक है, सबसे जुदा है और प्रेरणा देने की श्रमता रखने वाली है। ये सच्ची कहानी है डॉ पीवीएलएन मूर्ति की।

उनकी कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के बड़े शहर हैदराबाद से क़रीब साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर एक गाँव में। वही गाँव जहाँ मूर्ति का जन्म हुआ। मूर्ति का जन्म अविभाजित आंध्रप्रदेश के कर्नूल ज़िले के आल्लगड्डा में हुआ। मूर्ति अपने माता-पिता पंचर्ला पेद्दा दस्तगीरय्या और नागम्मा की पहली संतान थे। मूर्ति के बाद दस्तगीरय्या और नागम्मा को तीन बेटियाँ हुईं। पिता किसान थे और उनके पास पाँच एकड़ उपजाऊ ज़मीन थी। ख़ेत ही कमाई का एक मात्र ज़रिया थे। माता-पिता दोनों अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने अपनी सभी संतानों को ख़ूब पढ़ाने-लिखाने की ठानी। मूर्ति को आलगड्डा के भारतीय विद्या मन्दिरम् स्कूल में भर्ती कराया गया। अपने ख़ुद के खेतों से आमदनी इतनी नहीं थी जिससे बच्चे की पढ़ाई का ख़र्चा भी निकल पाता। बेटे मूर्ति की पढ़ाई जारी रहे और उसे कोई दिक़्क़त न आये इस वज़ह से दस्तगीरय्या और नागम्मा ने दूसरों के खेतों में जाकर मज़दूरी करना भी शुरू किया। मूर्ति छोटे थे लेकिन उन्हें ये अहसास था कि उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए उनके माता-पिता ख़ूब मेहनत कर रहे हैं। माता-पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने और उनके सपने साकार करने के मक़सद से मूर्ति ख़ूब मन लगाकर पढ़ने लगे। गाँव और घर में बिजली नहीं थी लेकिन मूर्ति ने कंदील की रोशनी में पढ़ाई की। और जब माँ चूल्हे पर खाना बनाती तब मूर्ति चूल्हे की आग से होने वाली रोशनी में पढ़ाई करते, सिर्फ़ इस वजह से कि कंदील का तेल बच जाय। उम्र में भले ही छोटे थे लेकिन समझ उनकी अच्छी थी। वे छोटी उम्र से ही खेत में जाकर अपने माता-पिता की मदद भी करने लगे थे। छोटे-छोटे हाथों से ही वे खेत से कूड़ा-कचरा उठाकर बाहर फेंकते।
मूर्ति ने पाँचवीं तक की पढ़ाई भारतीय विद्या मन्दिरम् स्कूल से की। इसके बाद उनके चाचा मूर्ति को अपने साथ कडपा ज़िले के लक्किरेड्डीपल्ली ले गये। चाचा की कोई संतान नहीं थी इसी वज़ह उन्होंने मूर्ति की पढ़ाई की ज़िम्मेदारी ली। लक्किरेड्डीपल्ली में मूर्ति ने ज़िला परिषद हाई स्कूल में पढ़ाई की। पाँचवीं से आठवीं तक यहाँ पढ़ाने के बाद उनके चाचा ने मूर्ति का दाख़िला कडपा शहर के श्री शारदा निलयम हाई स्कूल में करवाया। आठवीं तक मूर्ति ने तेलुगु में ही पढ़ाई-लिखाई की थी। नवीं से उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। ग्रामीण परिवेश से आने और आठवीं तक तेलुगु मीडियम स्कूल में पढ़ने की वज़ह से अंग्रेज़ी को अडॉप्ट करने में उन्हें काफ़ी तकलीफ़ें हुईं। लेकिन, लगन और मेहनत से तकलीफ़ों को दूर भगाया।
चूँकि मूर्ति पढ़ाई-लिखाई में तेज़ थे, मेहनत भी खूब करते थे, उनके पिता और चाचा को लगा कि वे डॉक्टर बन सकते हैं। इसी वज़ह से उनका दाख़िला कडपा के नागार्जुना रेजिडेंशियल स्कूल में कराया गया। उन्हें बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री यानी बीपीसी की क्लास में भर्ती किया गया।
इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने मूर्ति को ये प्रण लेने पर मज़बूर कर दिया कि उन्हें आगे चलकर डॉक्टर ही बनना है। हुआ यूँ था कि मूर्ति की दादी बीमार पड़ गयीं। इलाज़ के लिए बड़े अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए परिवारवालों के पास रुपये नहीं थे। इसी वज़ह से दादी को इलाज़ के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। मूर्ति भी अपनी बीमार दादी से मिलने अस्पताल आने-जाने लगे। न जाने दादी को क्या हुआ था वे सभी से कहने लगीं कि उनका पोता डॉक्टर है। अस्पताल के डाक्टरों से भी दादी यही कहतीं कि उनका पोता डॉक्टर है।

मूर्ति ने उन दिनों की यादें ताज़ा करते हुए हमें बताया,"पता नहीं दादी अचानक ऐसे क्यों कहने लगी थी।अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद पांचवें दिन ही उनकी मृत्यु हो गयी। लेकिन उनकी बातों का मुझपर बहुत असर हुआ।मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य डॉक्टर बनना ही हो गया।मुझे इस बाद का भी दुःख था कि डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाये थे कि दादी की बीमारी क्या है? उनकी तक़लीफ़ का कारण क्या है?"
इस घटना के बाद मूर्ति ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई-लिखाई की ओर लगा दिया। मूर्ति के मुताबिक,"ग्यारहवीं और बारहवीं की पढ़ाई के दौरान मुझे बहुत तक़लीफ़ हुई। मेरी स्कूली पढ़ाई तेलुगु मीडियम से हुई थी इसी वज़ह से बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के बड़े-बड़े शब्दों को, वो भी अंग्रेज़ी में याद रखना मुश्किल हो रहा था। अंग्रेज़ी को पूरी तरह से न समझ पाना बड़ी परेशानी थी। शुरू में तो मैं बहुत घबरा गया। लेकिन धीरे-धीरे पढ़ना शुरू किया। मुझे अहसास था कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो माता-पिता बहुत दुःखी होंगे। उनके सपने टूट जाएंगे। उनकी सारी उम्मीदें मुझ पर ही टिकी थीं। यही सोचकर मैं बस पढ़ता ही गया।"
मूर्ति ने बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की अंग्रेज़ी में किताबों को समझने के लिए एक तरकीब अपनायी। उन्होंने इन्हीं विषयों पर तेलुगु में लिखी किताबें भी ख़रीदी और इन किताबों के ज़रिये भी विषय-ज्ञान हासिल करने लगे। वे कहते हैं,"जहाँ दूसरे विद्यार्थी सिर्फ़ एक क़िताब पढ़ते थे वहीं मैं दो-दो क़िताबें पढ़ता था। डिक्शनरी भी हमेशा मेरे हाथ में रहती। जो कोई अंग्रेज़ी शब्द मेरी समझ में नहीं आता मैं तुरंत डिक्शनरी खोलकर उसका मतलब जान लेता। क़िताब पर पेंसिल से मैं अंग्रेज़ी शब्द के ऊपर उसका तेलुगु अनुवाद लिख देता था ताकि रिविशन के समय डिक्शनरी दुबारा न खोलनी पड़े।"
लेकिन दिन-रात की कड़ी मेहनत के बाद भी मूर्ति मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में ऐसा रैंक नहीं ला पाये जिससे उन्हें सीट मिल जाती। मूर्ति को तक़लीफ़ तो बहुत हुई लेकिन उन्होंने उम्मीदें नहीं छोड़ीं। हिम्मत नहीं हारी। मूर्ति ने अगले साल फिर से प्रवेश परीक्षा लिखने का फ़ैसला लिया। अच्छी तरह से तैयारी हो सके इस वज़ह से पिता ने उनका दाख़िला नेल्लूर के कोरा कोचिंग सेंटर में कराया गया। यहाँ उन्होंने पढ़ाई में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के लिए ख़ास ट्रेनिंग दी जाती थी। मूर्ति अच्छी तरह से जानते थे कि इस बार प्रवेश परीक्षा में नाक़ामी का सीधा मतलब था माता-पिता की सारी उम्मीदों पर पानी फेरना। माता-पिता मेहनत-मज़दूरी कर मूर्ति की पढ़ाई के लिए रूपये जुटा रहे थे। सुबह चार बजे उठकर माता-पिता काम करने चले जाते थे। ख़ूब मेहनत करते। उनके ऊपर अपनी तीन बेटियों की भी ज़िम्मेदारी थी। पूरी उम्मीदें, सारी आशाएँ मूर्ति पर ही टिक गयी थीं।

इस बार मूर्ति ने किसी को निराश नहीं किया। दूसरे एटेम्पट में उन्हें सीट मिल गयी। मूर्ति ने बताया,"मैं बहुत ख़ुश हुआ था। क़ामयाबी के पीछे दिन-रात की मेहनत थी। कोचिंग कॉलेज की पढ़ाई के बाद मैं अपने एक लेक्चरर के घर चला जाता ताकि विषय पर और भी पकड़ मज़बूत बना सकूँ। मेरे टीचर भी जान गए थे कि मुझ पर डॉक्टर बनने का जुनून सवार है। वे भी मेरी हर मुमकिन मदद करने लगे थे।"
इसी बातचीत के दौरान एक घटना का ज़िक्र करके मूर्ति बहुत ही भावुक हो गए। उन्होंने ये घटना सुनाकर पिता-बेटे के संबंध की गहराई और दोनों के बीच एक दूसरे पर विश्वास और उम्मीदों को बताने की कोशिश की। मूर्ति ने कहा,"जिस दिन मैं दूसरी बार प्रवेश परीक्षा लिखने वाला था उस दिन मेरे पिता गाँव से शहर आ गए थे। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि वे मेरे पास आने वाले हैं। वे तड़के ही शहर पहुँच गए थे लेकिन मेरे हॉस्टल नहीं आये। वे बस स्टॉप पर ही रुके रहे। उन्हें लगा कि अगर वे मेरे पास तड़के ही पहुँच गए तो मुझे तैयारी में परेशानी होगी। वे ठीक उस समय मेरे सामने आये जब मैं परीक्षा देने के लिए निकल रहा था। उन्हें देखकर मैं बहुत गदगद हुआ। मेरी ख़ुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो मेरे लिए हमेशा लकी रहे हैं। जब भी मैं उन्हें देखकर कोई भी परीक्षा देने गया हूँ मैं हमेशा पास हुआ हूँ। उन्हें देखते ही मुझे विश्वास हो गया कि इस बार मुझे हर हाल में सीट मिलेगी। जोश और विश्वास से भरे मन के साथ मैं परीक्षा देने गया और परीक्षा में बहुत अच्छा किया।" परीक्षा से पहले पिता को देखने पर विजयी होने का ये मनोभाव काम कर गया। मूर्ति ने अच्छा रैंक हासिल किया जिससे उन्हें एमबीबीएस की सीट मिल गयी।

मूर्ति को अपने गाँव से बहुत दूर विशाखापट्नम के आंध्रा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिली। मूर्ति बताते हैं कि आंध्रा मेडिकल कॉलेज के शुरुआती दिन बहुत ख़ौफ़नाक रहे। एक तो पहली बार वे अपने गाँव से इतनी दूर आये थे और दूसरा - यहाँ की बोली बिलकुल अलग थी। मेडिकल कॉलेज की यादगार घटनाओं की जानकारी देते हुए मूर्ति ने कहा,"मेरी जमकर रैगिंग भी की गयी। भाषा तेलुगु ही थी लेकिन मेरी बोली अलग थी। मैं रायलसीमा से था और यहाँ की बोली आँध्रप्रदेश के दूसरे जगहों से अलग है। दूसरे विद्यार्थी मेरी बोली को लेकर मज़ाक किया करते थे। शुरू में मुझे बहुत अटपटा लगा। क्लासरूम के बाहर की ये परेशानी तो मैं आसानी से झेल गया लेकिन क्लासरूम के अंदर बड़ी परेशानी थी। लेक्चरर जो पढ़ाते थे उसमें से कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। एमबीबीएस का कोर्स मुझे डरवाना लगने लगा। मोटे-मोटे, भारी भरकम शब्दों से मैं घबरा गया। मैं इतना घबरा गया कि मैंने ट्रेन पकड़ी और गाँव चला आया। मैंने पहली बार अकेले ट्रेन में इतना बड़ा सफ़र तय किया था। तब मैं गाँव पहुँचा और पिता को अपने गाँव आने का कारण बताया तो वे भी घबरा गए। उन्हें सदमा पहुँचा। लेकिन , जल्द ही वे इस सदमे से बाहर निकले और मुझे समझाया कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो सभी हमेशा ग़रीब ही रहेंगे और ज़िंदगी भर परेशानियाँ साथ रहेंगी। पिता ने मुझे अलग-अलग बातें कहकर समझाने की कोशिश की थी। मैं भी समझ गया कि घर-परिवार की भलाई के लिए मुझे मेडिकल कॉलेज वापस लौटना होगा।" मूर्ति वापस विशाखापट्नम लौटे और पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कॉलेज में उनके सीनियर्स ने उनकी बहुत मदद की। इस बातचीत में मूर्ति ये बताने से भी नहीं चूके कि उनके साथी उनकी कामयाबियों से जलते थे। क्लासमेट्स जानते थे कि मूर्ति ग्रामीण परिवेश से आये हैं और इसके बाद भी वे उनसे अच्छे नंबर ला रहे हैं इस बात को लेकर वे उनसे जलते थे। सीनियर्स से मूर्ति को लगातार मिलती मदद भी क्लासमेट्स की आँखों में खलती थी।
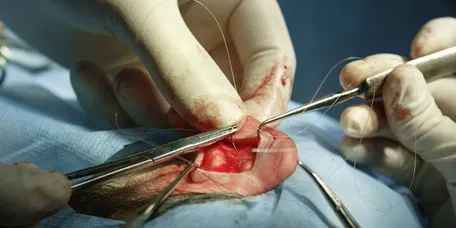
लेकिन मूर्ति ने इन सब की परवाह नहीं की और डॉक्टर बनने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी-जान लगा दिया। ग्रामीण परिवेश, अंग्रेजी भाषा जैसे कारणों की वजह से आईं तक़लीफ़ों को दूर भगाया। मेहनत और लगन क़ामयाब रही और मूर्ति ने 2000 में एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर ली।
एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान ही मूर्ति का मन सर्जरी पर आ टिका था। वे सर्जन बनना चाहते थे। उन्होंने प्लास्टिक सर्जन बनने के सपने देखे । मूर्ति ने कहा,"प्लास्टिक सर्जरी बड़ी चुनौतियों से भरा काम है। जलने की वजह से, या फिर, किसी और हादसे की वज़ह से बिगड़े हुए चहरे को प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिये जिस तरह फिर से चमकदार बनाया जा सकता है उसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। लेकिन, मैं प्लास्टिक सर्जन नहीं बन पाया। जिस तरह का रैंक था मेरा मुझे नाक, कान और गले वाले डिपार्टमेंट में भेजा गया।" मूर्ति को ईएनटी रोगों के इलाज़ में स्पेशलाइजेशन के लिए काकिनाडा के रंगराया मेडिकल कॉलेज में सीट दी गयी।
इसी बीच एक और ऐसी घटना हुई जिसने मूर्ति को फिर से घर-परिवार की ज़िम्मेदारियों की याद दिलायी। एक दिन पिता ने मूर्ति से पूछा, 'तुम डॉक्टर तो बन गए हो, फिर कब हमें तुम्हारी कमाई के रुपयों से भोजन का पहला निवाला मिलेगा।' पिता के इन शब्दों ने मूर्ति को हिलाकर रख दिया। मूर्ति जानते थे कि पिता ने उन्हें डाक्टर बनाने के लिए दिन रात एक किये थे। अपने खेतों के अलावा दूसरे के खेतों में भी पसीना बहाने के लिए मज़बूर किया था। मूर्ति के लिए दुविधा ये भी थी कि वे अपने पिता को समझा नहीं सकते थे कि स्पेशलाइजेशन के बाद ही उनकी कमाई शुरू होगी। और तो और दूसरे गाँव वाले पिता को ये कहकर टोंट भी मारते थे - तुम तो कहते हो तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया है फिर भी तुम मज़दूरी क्यों कर रहे हो ? तुम्हारा बेटा डॉक्टर बना भी है या नहीं ?

मूर्ति समझ गए कि ऐसे हालात में पिता को समझा मुश्किल हैं। इसी वज़ह से उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी करने की ठान ली। विशाखापट्नम में ही बच्चों के डॉक्टर राधा कृष्णा के यहाँ मूर्ति को डॉक्टरी की पार्ट-टाइम नौकरी मिल गयी। दिन में वे मेडिकल कॉलेज में ईएनटी स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई करते और शाम को डॉक्टर राधा कृष्णा के साथ मरीज़ों का इलाज़। मूर्ति ने बताया, " डॉ. राधा कृष्णा के साथ काम करने से मुझे कई फ़ायदे हुए। डॉ. राधा कृष्णा ने मुझे बच्चों के इलाज़ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दीं। बच्चों का इलाज़ कैसे किया जाता है ये बताया और सिखाया। यहीं पर काम करते हुए मुझ में बच्चों का इलाज़ करने में दिलचस्पी जगी। मैं एक तरह से बच्चों का डॉक्टर भी बन गया था। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि मेरी कमाई शुरू हुई। पढ़ाई का ख़र्च अब पिता को नहीं उठाना पड़ रहा था। पिता भी अब गाँववालों से कहने लगे थे - देखो, मेरा डॉक्टर बन गया है। वो कमाने भी लगा है और यही वज़ह से वो अब मुझसे रुपये भी नहीं लेता। "
ईएनटी में स्पेशलाइजेशन करने के बाद मूर्ति ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। वे अब कान-नाक और गले से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। मशहूर सर्जन हैं। बच्चों में कान-नाक और गले से जुडी समस्याओं को सुलझाने में माहिर हैं। वे इन दिनों दो बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।
डॉक्टर बनकर मूर्ति जब कमाने लगे तब उन्होंने घर-परिवार की कई ज़िम्मेदारियाँ अपने कंधों पर ले लीं। उन्होंने अपनी दूसरे बहन की शादी करवाई। तीसरी बहन की पढ़ाई में मदद की और इस मदद की वज़ह से वे आज आल्लगड्डा में डेंटल सर्जन हैं। पहली छोटी बहन की शादी पिता ने ही करवाई थी और मूर्ति उस समय इस हालत में नहीं थे कि वे पिता की मदद कर सकें। मूर्ति ने बड़ी ख़ुशी और बड़े फ़क्र के साथ हमें ये भी बताया कि अब उन्होंने अपने गाँव में एक बढ़िया मकान भी बनवा लिया है। वहाँ अब एसी भी है और गीज़र भी।
इस मुलाक़ात के दौरान मूर्ति ने हमें अपने डॉक्टरी जीवन की बड़ी ही यादगार और दिलचस्प घटनाओं के बारे में भी बताया। अपने पहले ऑपरेशन की यादें ताज़ा करते हुए मूर्ति ने कहा,"उन दिनों मेरी इंटर्नशिप चल रही थी। गले के कैंसर से पीड़ित एक मरीज़ आया था अस्पताल में। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने 'ट्राइकोस्टमी' की। मैंने ऑब्स्ट्रक्शन का बाईपास किया था ताकि बेहतर तरीक़े से मरीज़ साँस ले सके। मरीज़ को फ़ायदा भी मिलने लगा। अस्पताल में वो मरीज़ जितने दिन रहा उतने दिन मैंने उसकी ड्रेसिंग की और गले से निकलने वाले मैल आदि को साफ़ किया। ठीक होने के बाद वो मरीज़ अपने घर चला गया। एक दिन यही मरीज़ एक देशी मुर्गी लेकर अस्पताल आया और उसने मुझे ये मुर्गी दी। मुर्गी देते हुए उसने कहा - मैं ग़रीब हूँ। आपको कुछ दे नहीं सकता। आपने मेरी बहुत मदद की। मेरे पास मुर्गी थी। सोचा ये मुर्गी ही दे हूँ , इसी वज़ह से ये मुर्गी आपके लिए लाया हूँ। ये कहकर उस व्यक्ति ने मेरे हाथों में मुर्गी थमा दी और चला गया।" ख़ास बात तो ये थी कि जब उस व्यक्ति ने मूर्ति को कृतज्ञता भाव से मुर्गी दी थी उस समय अस्पताल में प्रोफ़ेसर, दूसरे डॉक्टर और कई सारे मरीज़ मौज़ूद थे। सभी ये घटना देखकर ख़ूब हंसें थे। मूर्ति ने बताया कि इस घटना के चार महीने बाद उस व्यक्ति की मौत हो गयी और उन्होंने उसकी पत्नी की आर्थिक मदद की थी।

अपनी ज़िंदगी के सबसे जटिल ऑपेरशन के बारे में भी मूर्ति ने हमें बताया। उन्होंने कहा," यमन से छह साल का एक बच्चा आया था। उसे भी सांस लेने में तक़लीफ़ थी। उसके माता-पिता उसे कई जगह ले गए थे। दो-तीन ऑपरेशन भी किये जा चुके थे। लेकिन बच्चे की तक़लीफ़ दूर नहीं हुई थी। बच्चे के माता-पिता को वो भाषा नहीं आती थी जो मैं समझता था। और मुझे वो भाषा नहीं आती थी जो वो बोलते-समझते थे। एक ट्रांसलेटर के ज़रिये मैंने उनसे उनके बच्चे की तक़लीफ़ के बारे में जाना। मुझे विश्वास था कि मैं बच्चे की तक़लीफ़ दूर कर सकता हूँ। मैंने ऑपरेशन किया और क़ामयाबी हासिल की। ऑपरेशन बहुत जटिल था। लेकिन मेरा अनुभव काम आया।"
मूर्ति ने ये भी बताया कि," बच्चों का ऑपरेशन हमेशा जटिल होता है। बच्चों में एयरवे छोटा होता है। हवा जाने की जो नली होती है वो बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होती है। लंग वाइटल कैपेसिटी और वॉल्यूम भी कम होता है।" उन्होंने इसी सन्दर्भ में आगे कहा," बड़े अपनी तक़लीफ़ बता सकते हैं , जबकि बच्चे अपनी तक़लीफ़ बता नहीं सकते। डॉक्टरों को ख़ुद उनकी तक़लीफ़ समझनी होती है। विशाखापट्नम में डॉ. राधा कृष्णा के साथ काम करते हुए मैंने बच्चों की तक़लीफ़ों को समझने की कला सीखी थी।"
डॉ. राधा कृष्णा ने अलावा मूर्ति डॉ श्रीनिवास किशोर को बहुत मानते हैं। वे कहते हैं, "डॉ श्रीनिवास किशोर मेरे बॉस हैं। उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पहली बार काम करने के बाद मुझे जो पहला चेक मिला था वो उन्होंने ही दिया था। मुझे वो दिन आज भी याद है और मैं उसे कभी भूल नहीं सकता।"
एक सवाल के ज़वाब में मूर्ति ने कहा," मेरी ज़िंदगी के दो तीन ही मक़सद हैं। पहला - ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा करूँ। दूसरा - ज्यादा से ज्यादा बच्चों की तक़लीफ़ें दूर करते हुए उनकी ज़िंदगी में ख़ुशियाँ लाऊँ। तीसरा - माता-पिता की सेवा करूँ और पत्नी-बच्चों को ख़ुश रखूं।"
मूर्ति से इस बातचीत के दौरान कई बार एहसास हुआ कि वे उनके पिता से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। पिता उनकी सबसे बड़ी और अमूल्य संपत्ति हैं। एक संदर्भ में मूर्ति ने कहा, "मेरी कामयाबियों पर पिता ख़ुश बहुत होते, लेकिन अपनी ख़ुशी का इज़हार मेरे सामने नहीं करते। लेकिन वे अपनी ख़ुशी दूसरे सामने ज़ाहिर करते थे। दूसरों से ही मुझे पता लगता था कि वे कितने ख़ुश हैं। मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मुझ में अहंकार आ जाए। उन्हें लगता था कि अगर वे मेरे सामने मेरी तारीफ़ कर दें तो मुझमें अहंकार आ जाएगा। एक बात है जो वो मुझसे कई बार कहते, वे कहते- कभी भी अपने आप को महान मत समझो। ये मत समझो कि काम ख़त्म हो गया है। अभी बहुत काम करना बाकी है। दुनिया में बहुत सारा काम है जो तुम्हें करना है।"