कभी साइकिल गिरोह के साथ मुफ्त फिल्में देखते थे आज के सफल धारावाहिक लेखक डॉ. बोधिसत्व
उत्तर प्रदेश के दो मशहूर शहर वाराणसी से 61 किलोमीटर और इलाहबाद से 90 किलोमीटर की दूरी पर भदोही के निकट एक छोटे से गाँव भीखारीपुर में एक लड़का, अपने साथियों के साथ सारे इलाके में शरारतपूर्ण गतिविधियों में सक्रिय रहता है। घर से कॉलेज के बीच 15 किलोमीटर के दायरे में दोस्तों के साथ साइकिलों पर घूमना, मुफ्त में फिल्में देखना, पार्किंग का पैसा न देना और बिना पैसे के समोसे और जिलेबी की उगाही करना, इन सब गतिविधियों के बीच दो तीन साल में वह 265 फिल्में देखता है और घर पहुँचकर इन फिल्मों की पटकथा, गीत, संवाद और फिल्मनिर्माण से जुड़ी टीम की संपूर्ण जानकारी अपनी कापी के पन्नों पर उतारता है। उस 18 से 20 वर्ष आयु के युवक अखिलेश कुमार मिश्र को यह बिल्कुल नहीं मालूम था कि वह एक दिन टीवी धारावाहिकों का सफल लेखक बनेगा। यह कहानी डॉ. बोधिसत्व की है। बोधिसत्व के लिखे कई धारवाहिक लोकप्रिय हो चुके हैं। इसके बावजूद एक फ्रीलांस लेखक की चुनौतियों को वे हर दिन जीते हैं।
डॉ. बोधिसत्व ने अपने बचपन में यह तो ज़रूर सोचा था कि उन्हें लोकप्रिय होना है, लेकिन टेलीविजन और फिल्मों के लेखन द्वारा प्रसिद्धि मिलेगी यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने आमृपाली, 1857 क्रांति, शंकुंतला, रेत, जय हनुमान, कहानी हमारे महाभारत की, देवों के देव महादेव जैसे कई धारावाहिक लिखे और शिखर जैसी फिल्म का लेखन भी किया। अखिलेश मिश्र उर्फ बोधिसत्व बचपन में काफी घुमक्कड और शरारती किस्म के लड़के थे। हालाँकि उनके घर में शिक्षा पहले से थी, लेकिन उनका मन स्कूल की शिक्षा पढ़ने में कम और इधर-उधर भटकने में अधिक लगता। ऐसा नहीं कि उन्हें पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन वो उन किताबों की ओर अधिक आकर्षित होते, जो अलमारियों में रखी हैं, जो बड़े लोग पढ़ते हैं। इन्हीं किताबों और पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हुए ही उनके मनमें छपने की इच्छा जागी। वे कहते हैं,
- मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी कि मेरा नाम छपा हुआ देखूँ। चाहे वह मैय्यत या उठावने में भाग लेने वाले लोगों में ही क्यों न हो। लोग मुझे जानें। साहित्य में माना जाता है कि प्रसिद्धि की कामना मन में होना चाहए। यही रास्ता देती है आगे पढ़ने के लिए। चौथी पाँचवीं में मैंने निर्मला पढ़ ली थी, फिर रामचरित मानस, रामायण, भागवत, ऐसी किताबें घर में उपलब्ध थीं। हम बच्चे उसमें से नकली चौपाइयाँ बना कर दूसरे बच्चों को अंताक्षरी में हराते थे। हम जीत रहे थे, लेकिन कैसे जीत रहे थे, वे हमें ही मालूम था।

बोधिसत्व अपने स्कूल के एक मास्टर से मिली प्रेरणा के बारे में बताते हैं, - स्कूल में लक्ष्मी प्रसाद उपाध्याय अंग्रेजी के टीचर थे, लेकिन वो अंग्रेज़ी पढ़ाने के अलावा सब कुछ पढ़ाते थे। वे बे औलाद थे। हमारे पास बे औलाद का मतलब ये होता था कि उन्हें केवल बेटियाँ हैं, पुत्र नहीं हैं। हर शनिवार को एक सांस्कृतिक आयोजन करते थे, जिसमें हर बच्चा एक कविता सुनाता था। मैंने भी एक कविता सुनाई, तो उन्होंने उसकी सराहना की। `आज' और `ओज' पत्रिकाओ़ं में उनकी कुछ कविताएँ छपती रहती थीं। मेरे ताऊजी के लड़के भी तरही शायरी करते थे। मुद्दतों मैंने सिनेमा के गानों के आधार पर असंख्य गाने लिखे। गाँव में उर्दू का अच्छा माहौल था। कसम और तलाक शब्द काफी प्रचलित थे। तलाक से हम दोस्ती तोड़ते थे और बात बात पर अल्लाह की कसम खाते थे।
किताबें पढ़ने और कविताएँ लिखने के बावजूद, स्कूली शिक्षा में उनकी रूची कम होने के कारण इंटर और डिग्री की परीक्षा में उन्होंने मुश्किल से कामयाबी हासिल की। डिग्री के दौरान की गयी शरारातों का उल्लेख करते हुए बोधिसत्व बताते हैं,
- बात 1984 के आस-पास की है। पढने का कोई माहौल तो था नहीं। बारह पंद्रह बच्चे साइकिल चला कर 10 पंद्रह किलोमीटर तक पढ़ने जाते थे। चार पाँच किलोमीटर के दायरे में चार-पाँच सिनेमा हाल थे। कॉलेज जाना हाज़री लगाना और फिर सिनेमा हालों की ओर निकल जाना, सिनेमा में बिना टिकट का सिनेमा देखना, बिना पैसे से साइकिल स्टैंड पर साइकिल रखना, बाहर निकलते हुए दुकानों से एक एक समोसा और दो दो जेलेबी की उगाही करना, हमारा रोज़ाना का मामूल बन गया था। दो वर्षों के अंतराल में मैंने 265 फिल्में देखी। जब नई फिल्म नहीं लगती तो पुरानी ही देख लिया करते थे। नदिया के पार मैंने पाँच बार देखी थी। मैं फिल्म देखता ही नहीं था, बल्कि उसकी संपूर्ण जानकारी भी रखता था। कापी के पन्ने के एक तरफ फिल्म के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, गीतकार, लेखक, गीत कहानियाँ आदि सभी प्रकार की जानकारी लिख दिया करता था। दसवीं तक तो स्थिति किसी तरह ठीक थी, लेकिन बारहवीं में थर्ड डिविजन में पास हुआ। डिग्री में भी यही हाल था। कैंम्पस नहीं जाना, टीचर से झगड़े करना, नहीं पढूंगा कहके निकल जाना और इलाहबाद में घूमते रहना, चलता रहता। ऐसा नहीं था कि पढ़ने में दिलचस्पनी नहीं थी, क्लास में अगर उस दिन बिहारी, या तुलसी को पढाया जाना है तो मैं नहीं बैठता था, क्यों कि इनको को तो मैं पहले ही पढ़ चुका था। पहले एक छात्र क्लास से बाहर निकलता था, फिर पाँच छह उसके पीछे निकल जाते थे। इस तरह मैं कभी भी मित्र विहीन नहीं रहा हूं। भदोही छूटा तो इलाहबाद में भी यही सब कुछ हुआ करता था, जाड़ों में रात भर साइकलिंग करना, धूप में लू में रूमाल मूँह पर बाँध कर निकल जाना। कोई रोकने वाला नहीं था।

ऐसा नहीं कि वे केवल शरारतों में ही व्यस्त रहे। जब पढ़ने पर आये तो एम ए में टॉप किया और जेआरएफ की छात्रवृत्ति हासिल कर पीएचएडी की उपाधि भी प्राप्त की। रामायण और महाभारत के कई संस्करण पढें थे। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात अपने दौर के विख्यात कवि उपेंद्र नाथ अश्क से हुई। उस घटना का उल्लेख करते हुए बताते हैं,
- अख़बार में उपेंद्र नाथ अश्क का एक इंटरव्यू छपा था। उसमें उन्होंने कहा था कि वे नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देंगे। समाचार पत्र में अन्ना हज़ारे टाइप की एक तस्वीर छपी थी। मैंने सोचा कि यह देवदूत मुझे बढ़ावा देगा। मैंने उनकी तरह की एक टोपी और कुर्ता पाइजामा खरीदा और वही पहन कर उनके एड्रेस पर खुसरो बाग पहुँच गया। मैंने वहाँ जाकर उनका पता पूछा तो एक व्यक्ति ने जो कुछ कहा, मेरे लिए आश्चर्चयकित कर देने वाला था, उसने कहा, वह पगलवा..उसका घर तो दीवार के उस तरफ है। मई जून की धूप थी। उन्होंने मुझे देखा तो कहा...गुस्सा छोड़ दो तो अश्क जी मिलेंगे। ... क्रोध पाप का मूँह है।...यह कहते हुए खुद ही सुराही का पानी पिलाया। मेरी आठ दस कविताएँ सुनीं। एक कविता चुनी और कहा इस पर काम करो। मैंने एक कविता सुनाई। उन्होंने कहा..इसमें से कुछ टुकड़ें अच्छे हैं। इस पर कुछ काम करो। मैंने काम का मतलब यही समझा कि उसे अच्छे से लिखना है और उसे फिर से सुलेख में लिख दिया, उन्होंने फिर कहा कि इसपर काम करो। फिर उन्होंने खुद ही उस कविता को सुधारा, संवारा। मेरे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने मेरी कविता को शीर्षक दिया। वो पन्ने मेरे पास आज भी हैं। ...अपने आप बोल उठता हूँ जैसे, बोल उठता है हवा में उडता सूखा पत्ता.. मैं तीन वर्षों तक उनके संपर्क में रहा।
- फिर अश्नेक जी ने चार अध्यापकों के नाम दिये। उनके बाद मैं दूधनाथ सिंह के संपर्क में रहा। दूधनाथ सिंह ने दस कविताएं चुनीं और उस जैसी मैंने 70 अस्सी कविताएँ लिखीं। उन्होंने कहा जिस विषय को एक बार लिखा है, उसे दोबारा मत लिखो। उन कविताओं में से उन्होंने आलोचना पत्रिका को 40 कविताएँ भेजीं, 14 नामवरजी ने छापी, 5 कविताएं मंगलेश डबराल को दी, जो उन्होंने जनसत्ता में प्रकाशित कीं, उन्होंने सोमदत्त को दीं इस तरह बची हुई कविताएँ 'स्वतंत्र भारत' और 'चौथी दुनिया' में प्रकाशित हुईं। तीन महीने में 45 कविताएं छपी। यह मेरे लिए बड़ी बात थी। कविताएं पढ़ कर कुछ लोग मानते थे, कि कोई बूढा होगा कि जो बोधिसत्व के नाम से छपता था।
अखिलेश मिश्र से डॉ. बोधिसत्व बनना भी बड़ा दिलचस्प रहा। उन्होंने बताया कि एक लेखक तद्भव नामक पत्रिका निकालते थे। उनका नाम भी अखिलेश था।इनकी कविताओं को पढ़कर कुछ लोगों ने उनकी ताराफी कर दी और कुछ लोगों ने इन्हें कहानीकार समझ लिया। उनके कहने पर ही अखिलेश कुमार मिश्र ने नये नाम की तलाश शुरू की और फिर शिल्परत्न, शाली होत्री, धूसर, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध और वज्रपान सहित दस फाइनल किये। आखिरकार गौतमबुद्ध नाम तय हुआ,लेकिन उसी नाम की जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें बोधिसत्व नाम मिला और यही उपनाम उनकी पहचान बनकर रह गया।
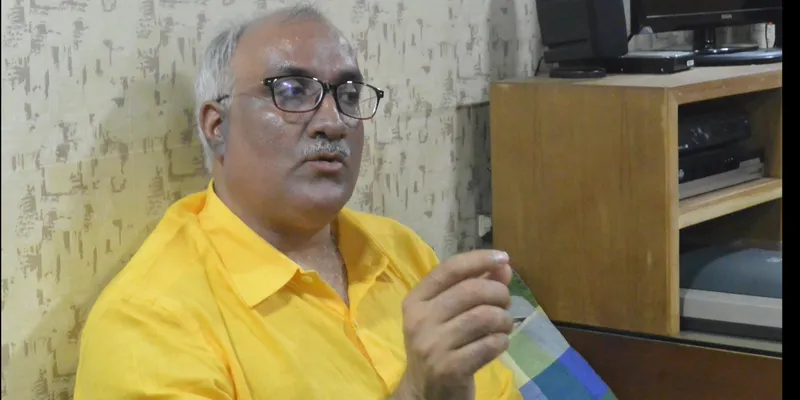
उन्हीं दिनों बोधिसत्व ने अमर उजाला के लिए भी काम किया। उन दिनों के बारे में वे बताते हैं कि वह बड़ा संघर्षों से भरा दौर था। फेलोशिप के रुपये बस नहीं होते थे। इसलिए एक ऐसी नौकरी की ज़रूरत थी, जहाँ 3000 हज़ार रुपये मिल सकें। अमर उजाला में वह मिल गये। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यालय में भी उन्होंने काम किया। तीन साल तक सिलेबस समिति के सदस्य और म्युजियम के निदेशक सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया और एक दिन अचानक मुंबई की फिल्म और टेलीविजन की दुनिया ने उन्हें बुला लिया। जी टीवी में गौतमबुद्ध पर एक शो बनाने के लिए चार महीने की छुट्टी लेकर मुंबई गये तो वे फिर मुंबई ही के होकर रह गये। इस बीच लेखकों की मूल पाँडुलीपियाँ जुटाने का काम भी उन्होंने किया। वे कहते हैं,
- मेरी ज़िंगदी में बेरोज़गारी मित्र की तरह रही। कभी तो दो लाख रुपये कंपनी ने दिये, लेकिन काम कुछ नहीं था। संयोग था कि उन्हीं दिनों साहित्य अकादमी में काव्य पाठ के लिए बुलाया गया था। परसों काव्यपाठ था और आज चिट्ठी आयी थी, जाएं कैसे...भाई ने कहा प्लेन से चले जाओ। मिलने वाले थे 3600 रुपये, लेकिन आने जाने के 24 हज़ार रुपये, खैर चला गया। प्लेन में बगल वाली सीट पर संजय खान बैठे थे, उन्हीं दिनों उनका एक शो शुरू हुआ था, मैंने आव देखा न ताव उन पर बरस पड़ा।
... आपके शो में इतना झूठ क्यों चलता रहता है...आप 1849 में कानपूर में ट्रेन उडा रहे हैं...बोरी बंदर से ठाने के बीच 1851 को पहली ट्रेन चली थी और उत्तर भारत में तो 1883 के आस पास आयी थी। ..... वे सुनते रहे और फिर अपना कार्ड देकर मुंबई में मिलने के लिए कहा। इस तरह हर मोड पर बोधिसत्व को कई लोग मिले। संजय खान के साथ उन्होंने तीन साल तक काम किया और फिर बेरोज़गार हुए तो फिर नयी डगर पर चल पड़े। फिल्म और टेलीविजन के लिए लिखना सीखने के लिए उन्होंने स्वाध्याय किया। गंगा जमुना, शोले, देवदास, दो बीघा ज़मीना जैसी कई फिल्में देखकर उनकी पूरी स्क्रिप्ट अपनी कापियों पर उतारी। अपने इस जीवन के बारे में वे कहते हैं,
- मैं अपने को कमायाब तो नहीं मानता, लेकिन मैं असफल भी नहीं मानता। कामयाबी की अवधारनाएँ अलग- अलग हैं। अभी दो फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी हैं, निर्माता निर्देशक का इंतेज़ार है। पैसा कमाना अगर कामयाबी है तो मैं कामयाब हूँ। मैंने कुछ खोया नहीं है।
टेलीविजन और फिल्म लेखन में वे काफी अंतर मानते हैं। उनका मानना है कि टेलीविजन बक बक के समान है, वह असीमित है। कोई विषय कितना भी लंबा खींचा जा सकता है, लेकिन फिल्म उस कविता के समान है, जो सीमित है। टीवी में हर अगले एपिसोड में कहानी बदली जा सकती है, लेकिन फिल्म में ऐसा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि सिनेमा में लिखना चुनौतीपूर्ण है। वहाँ पचास साठ पन्नों में कही जाने वाली बात को 15 से 20 सेकेंड में कह देना होता है। दर असल सिनेमा साहित्य को अमीर बनाता है। वह साहित्य में बाधक नहीं होता। कुछ अच्छा करने के उकसाता है। अपने इन्हीं विचारों के कारण वे साहित्य, टेलीविजन और सिनेमा में बने हुए हैं।
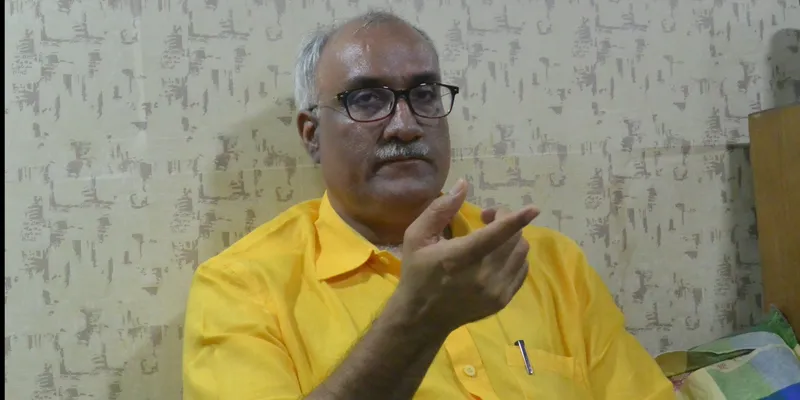
सिनेमा और टेलीविजन में एक लेखक के लिए आज भी सफलता के बाद कब असफलता मिले और कितनी देर सफलता का इंतेज़ार करना पड़े पता नहीं रहता। बोधिसत्व इन चुनौतियों का उल्लेख करते हुए अपने पुराने दिन याद करते हुए कहते हैं,
- मेरे लिए मुश्किलें कभी आयीं तो वह आर्थिक रूप से ही आयीं, लेकिन दोस्तों की मदद से हल होती गयीं। वैसे मुझे किसी से उधार मांगना सबसे मुश्किल काम लगता है और उधार मांगने वाले से ना कहना उतना ही मुश्किल लगता है। मुझे हर हाल में जीने की आदत है। हालाँकि कपड़े और किताबें मेरा शौक रही हैं, लेकिन बचपन में मैंने भाइयों की उतरने पहनीं हैं, ग्रैज्वेशन तक मेरे पास एक दो कपड़े ही नये हुआ करते थे। भाइयों के कपड़े उतरते रहते, कमर टाइट करके पहना करता था। जब संजय खान के पास तीन साल तक काम करने के बाद अचानक पता चला कि उनका प्रोडक्शन बंद हो रहा है तो कमरे में एक कोने में बैठकर देर तक रोया था, लेकिन फिर ज़िंदगी शुरू हुई और कई लोगों के पास घूमता रहा, फिर काम मिलता रहा।
डॉ. बोधिसत्व का मानना है कि कोई भी समय ऐसा नहीं होता जब आप हार के बैठ जाएँ, बल्कि नाउम्मीदी एक बडा धोखा होती है। बुरे वक़्त में ही इन्सान का सही इम्तेहान होता है। अच्छे समय में कोई इम्तेहान नहीं होता। इसलिए आदमी को अपने बुरे वक़्तों में परेशान होने के बजाय उससे सीखना चाहिए।







