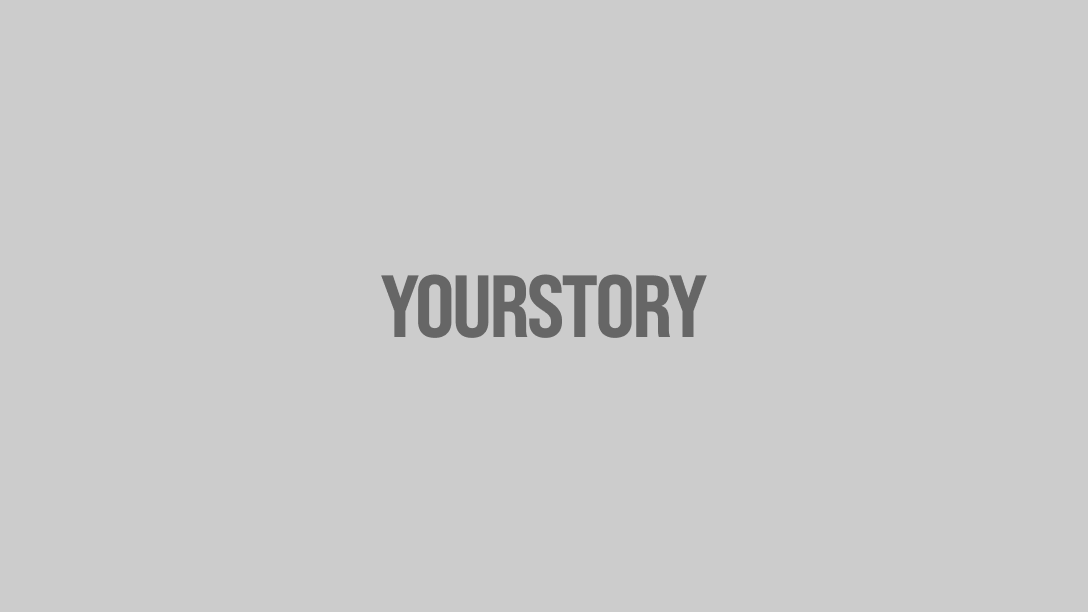रामदेव धुरंधर ने पहले कुदाल उठाई फिर कलम
हिंदी के शीर्ष प्रवासी साहित्यकार रामदेव धुरंधर को शब्द-संघर्ष विरासत में मिला है। उन्हें 'श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान' से समादृत किया गया है। उनका जीवन पथरीले-कंटीले रास्तों पर चल का आज इतना सशक्त हुआ है कि वह हिंदी के यशस्वी साहित्यकारों में शुमार होते हैं। उनकी एक दर्जन से अधिक कृतियां उपन्यास, कहानी संग्रह, लघु कथा संग्रह आदि प्रकाशित हो चुके हैं।

रामदेव धुरंधर (फोटो साभार- सोशल मीडिया)
मारिशस के कवि भारतीय संस्कारों के प्रति विशेष निष्ठावान हैं। बदलते मूल्यों से तालमेल बिठाना कठिन है। ठाकुरदत्त पांडेय इस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। शोषण के बदलते संदर्भ और हथियार के बारे में अनत का कहना है।
हिंदी के शीर्ष प्रवासी साहित्यकार रामदेव धुरंधर को ग्यारह लाख रुपए के 'श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान' से समादृत किया गया है। वह मॉरिशस में रहते हैं लेकिन वहां के अन्य रचनाकारों की तरह उनका भी मन भारत की मिट्टी में रचा बसा रहता है। उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के रहे हैं। 'श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफको साहित्य सम्मान' से अब तक विद्यासागर नौटियाल, शेखर जोशी, संजीव, मिथिलेश्वर, अष्टभुजा शुक्ल, कमलाकान्त त्रिपाठी आदि को सम्मानित किया जा चुका है। धुरंधर का चर्चित उपन्यास 'पथरीला सोना' छह खंडों में प्रकाशित है। इस महाकाव्यात्मक उपन्यास में उन्होंने किसान-मजदूरों के रूप में भारत से मारीशस गए अपने पूर्वजों की संघर्षमय जीवन-यात्रा का कारुणिक चित्रण किया है। इसके अलावा उनकी 'छोटी मछली बड़ी मछली', 'चेहरों का आदमी', 'बनते बिगड़ते रिश्ते', 'पूछो इस माटी से', 'विष-मंथन', 'जन्म की एक भूल' आदि कृतियां भी प्रकाशित हो चुकी हैं।
उनका विपुल साहित्य पूरी तरह किसानों के जीवन पर केन्द्रित रहा है। 'पथरीला सोना' अपने आप में एक महाख्यान है। धुरंधर लिखते हैं - 'मोरिशस के हिन्दी साहित्यकारों को व्यंग्य लेखक बनने की सनक पालनी नहीं चाहिये। मैंने पाल ली तो पाल ली, अतः वाहवाही मेरी, धुनाई भी मेरी। आप साहित्यकार जहाँ हैं, वहीं जमे रहिये। कविता का बाज़ार मंद पड़ा हुआ है, सिर पर मार कर फाटक तोड़िये ताकि कविता सदाबहार लूट सके। प्रेम कहानी लिखने वाले पता नहीं कहाँ खोये हुए हैं। कहानी न होती हो प्रेम की भाषा कौन बोलेगा? भुक्कड़ गली अथवा सभा सोसाइटी में प्रेम-प्रेम तो रटा जा रहा है, लेकिन प्रेम कहानी के अभाव में प्रेम ही सुन्न है।'
डॉ लता लिखती हैं कि मारिशस बाहरी देशों के निवासियों के द्वारा बसाया गया देश है। यही कारण है कि प्रत्येक प्रवासी अपने देश के संस्कारों से जुड़कर लिखता रहा है। बड़ी-बड़ी शास्त्रीय परिभाषाओं और वादों के मानदंडों पर यहाँ के हिन्दी काव्य को जाँचना अन्याय होगा। यहाँ लोगों ने हिन्दी में काव्य सृजन के उद्देश्य से कविताएँ लिखी हैं। अभी तक एक भी महाकाव्य या खंडकाव्य यहाँ के कवियों ने नहीं लिखा है। यहाँ के कवियों की बंधी कलम से अब तक यह सम्भव भी नहीं था पर भविष्य का क्षितिज आशा की अरुणिमा लिए हुए है। मारिशस के कवि विषय और शिल्प दोनों के प्रति सतर्क हैं। जहाँ संतुलन है वहाँ रचना उत्कृष्ट है। इनकी रचनाओं में आशा, आस्था और विश्वास के स्वर प्रमुख हैं।
मारिशस के कवि भारतीय संस्कारों के प्रति विशेष निष्ठावान हैं। बदलते मूल्यों से तालमेल बिठाना कठिन है। ठाकुरदत्त पांडेय इस संदर्भ में उल्लेखनीय हैं। शोषण के बदलते संदर्भ और हथियार के बारे में अनत का कहना है। मॉरिशस में उपन्यास के विकास के लिए जितनी परिस्थितियाँ, संस्कृतियाँ और विषय हैं, उस अनुपात में उपन्यास का विकास नहीं हुआ है। 1980 तक कुल पंद्रह उपन्यास लिखे गए हैं। रामदेव धुंरधर का शिल्प कैमरे से खींचा गया चित्र सा लगता है।
'जन्म की एक भूल' रामदेव धुरंधर का द्वितीय कहानी संग्रह है। ज्यादातर वे नाटक, लघुकथा और उपन्यास में अपनी लेखकीय निष्ठा का अर्घ्य समर्पित करते रहे। पर कहानी लेखन की उनकी बेचैनी यथावत् बनी रही। उसी बेचैनी का परिणाम 'जन्म की एक भूल' कहानी-संग्रह के रूप में पाठकों के समक्ष है। प्रस्तुत संग्रह में कुल सत्रह कहानियाँ संकलित हैं। हर कहानी का अस्तित्व एक दूसरी से पृथक् है। रामदेव धुरंधर बताते हैं कि भारतीय मज़दूरों का पहला जत्था सन् 1834 में मॉरिशस लाया गया था। मेरे पिता का जन्म - वर्ष 1897 था। प्रथम भारतीयों का मॉरिशस आगमन और मेरे पिता के जन्म के बीच लगभग छह दशक का फासला है। तब भी भारत से लोगों को इस देश में लाया जाना ज़ारी था।
इस दृष्टि से मेरे पिता मेरे लिए इतिहास के सबल साक्षी थे। भारतीयों को लाकर गोरों की ज़मींदारी के झोंपड़ीनुमा घरों में बसाया जाता था। तब भारतीयों के दो वर्ग हो जाते थे। एक वर्ग के लोग वे होते थे जिन्हें जहाज़ से उतरने पर गोरों की ओर से बनाये गये झोंपड़ीनुमा घरों में रखा जाता था। वे गोरों के बंधुआ जैसे मज़दूर होते थे। दूसरे वर्ग के लोग वे हुए जो भारत से सब के साथ जहाज़ में आते थे, लेकिन काट-छाँट जैसी नीति में पगे होने से वे गोरों के खेमे में चले जाते थे। वे सरदार और पहरेदार बन कर अपने ही लोगों पर कोड़े बरसाते थे।
विस्थापन का दर्द तो उन अतीत जीवियों का हुआ जो इस के भुक्तभोगी थे। मैं उन लोगों के विस्थापन वाले इतिहास से बहुत दूर पड़ जाता हूँ परंतु मैं पीढ़ियों की इस दूरी का खंडन भी कर रहा हूँ। उन लोगों का विस्थापन मेरे अंतस में अपनी तरह से एक कोना जमाये बैठा होता है और मैं उसे बड़े प्यार से संजोये रखता हूँ। इसी बात पर मेरा मनोबल यह बनता है कि मैं भारतीयों के विस्थापन को मानसिक स्तर पर जीता आया हूँ। यहीं नहीं, बल्कि मैं तो कहूँ अपने छुटपन में मैं अपने छोटे पाँवों से इतिहास की गलियों में बहुत दूर तक चला भी था।
रामदेव धुरंधर अपने पिता से सुनी आपबीती से संस्कारित हुए। भारतीयों का दुख-दर्द उनकी धमनियों में बहुत गहरे उतरता रहा था। वह तो बाद की बात थी कि वह लेखक हो गए परंतु संभवतः उनके पिता अप्रत्यक्ष रूप से उन्हे लेखन कर्म के लिए तैयार करते रहे थे। वह उनके लिए अच्छी कलम खरीदते थे। यद्यपि उनके पिता अनपढ़ थे, लेकिन पाटी, पुस्तक और पढ़ाई के दूसरे साधनों का वह उन्हें कभी अभाव नहीं होने देते थे। उन्हें ज्ञात था सरस्वती नाम की एक देवी है जिस के हाथों में वीणा होती है और उसे विद्या की देवी कहा जाता है। उनके पिता ने सरस्वती का कैलेंडर दीवार पर टांग कर किसी दिन उनसे कहा था कि विद्या प्राप्ति के लिए नित्य उसका वंदन किया करें। वह एक साल के लिए कैलेंडर था, लेकिन उसे मूर्ति मान कर घर से कभी हटाया नहीं गया।
वर्षों बाद जब उनका नया घर बना तो सरस्वती की नई स्थापना की गई थी। धुरंधर ने विभिन्न विधाओं में कलम चलाई है। वह बताते हैं कि मैंने ‘इतिहास का दर्द’ शीर्षक से एक नाटक (1976) लिखा था, जो पूरे देश में साल तक विभिन्न जगहों में मंचित होता रहा। यह पूर्णत: भारतीयों के विस्थापन पर आधारित था। मेरे लिखे शब्दों को पात्र मंच पर जब बोलते थे, मुझे लगता था, ये प्रत्यक्षत: वे ही भारतीय विस्थापित लोग हैं जो मॉरिशस आए हैं और आपस में सुख-दुख की बातें करने के साथ इस सोच से गुजर रहे हैं कि मॉरिशस में अपने पाँव जमाने के लिए कौन से उपायों से अपने को आजमाना ज़रूरी होगा।
रामदेव धुरंधर कहते हैं कि अपने लेखन के लिए मैंने भारतीयों का विस्थापन लिया तो यह अपने आप सिद्ध हो जाता है, मैंने उनके सुख-दुख, आँसू, शोषण, गरीबी, रिश्ते सब के सब लिए। मैंने लिखा भी है, मैं आप लोगों के नाम लेने के साथ आप की आत्मा भी ले रहा हूँ। मैं आप को शब्दों का अर्घ्य समर्पित करना चाहता हूँ, अत: मेरा सहयोगी बन जाइए। उनसे इतना लेने में हुआ यह कि मैं भी वही हो गया, जो वे लोग होते थे। किसी को आश्चर्य होना नहीं चाहिए अपने देश के इतिहास पर आधारित अपना छ: खंडीय उपन्यास ‘पथरीला सोना’ लिखने के लिए जब मैं चिंतन प्रक्रिया से गुजर रहा था, तब मैं उन नष्टप्राय भित्तियों के पास जा कर बैठता था, जिन भित्तियों के कंधों पर भारतीयों के फूस से निर्मित मकान तने होते थे।
ये मकान उनके अपने न हो कर फ्रांसीसी गोरों के होते थे। उन मकानों में वे बंधुआ होते थे। मैंने उन लोगों से बंधुआ जैसे जीवन से ही तारतम्य स्थापित किया और लिखा तो मानो उन्हीं की छाँव में बैठ कर। बात यह भी थी कि भारतीयों के उन मकानों या भित्तियों का मुझे चाहे एक का ही प्रत्यक्षता से दर्शन हुआ हो, अपनी संवेदना और कल्पना से मैंने उसे बहुत विस्तार दिया है। तभी तो मुझे कहने का हौसला हो पाता है। मैंने उसे भावना के स्तर पर जिया है। पर्वत की तराइयों के पास जाने पर मुझे एक आम का पेड़ दिख जाए तो मेरी कल्पना में उतर आता है। मेरे पूर्वजों ने अपने संगी साथियों के साथ मिल कर उन्हें रोपा था। मेरे देश में तमाम नदियाँ बहती हैं जिन्हें मैंने मिलाकर मनुआ नदी नाम दिया है।
इसी तरह पर्वत यहाँ अनेक होने से मैंने बिंदा पर्वत नाम रख लिया और आज मुझे सभी पर्वत बिंदा पर्वत लगते हैं। मैंने सुना है, दुखों से परेशान विस्थापित भारतीयों की त्रासदी ऐसी भी रही थी कि पर्वत के पार भागते वक्त उन के पीछे कुत्ते दौड़ाये जाते थे। कुआँ खोदने के लिए भेजे जाने पर ऊपर से पत्थर लुढ़का कर यहाँ जान तक ली गई हैं। बच्चे खेल रहे हों और कोई गोरा अपनी घोड़ा बग्गी में जा रहा हो तो आफ़त आ जाती थी। यह न पूछा जाता था कि स्कूल क्यों नहीं जाता। कहा जाता था कि बड़े हो गए हो तो खेतों में नौकरी करने क्यों नहीं आते हो पर ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में यह लिखित मिलने की कोई आशा न करे, क्योंकि लिखने की कलम उन दिनों केवल फ्रांसीसी गोरों के पास रहती थी।
धुरंधर के शब्दों में जो इंसानियत की लौ धधकती है, जो आवाज गूंजती है, उसका धरातल उनके जीवन का कठिन संघर्षों से उपजा है। वह बताते हैं कि मेरी पढ़ाई व्यवस्थित रूप से न हो सकी तो इस का कारण घर का बँटवारा था। दोनों बड़े भाइयों की शादी होने पर वे अपने कुनबे की चिंता करने लगे थे। उनके अलग होने पर हम माता-पिता और तीन बच्चे साथ जीने के लिए छूट गए। यहाँ भी वही हुआ। हमें जीना था तो हम जी लिये। यहीं मुझे मज़दूरी करने के लिए कुदाल थामनी पड़ी जो वर्षों छूटी नहीं। इस बीच पिता बीमार हुए तो स्वस्थ हो पाना उनके लिए स्वप्न बन गया और आखिरकार वह दुनिया से चले गए। धुरंधर को बचपन में पिता से ही हिन्दी का संस्कार मिला। हिन्दी का ज्ञान उन्होंने बाद में जैसे तैसे अर्जित किया।
हिन्दी प्रचारिणी सभा के सौजन्य से वह व्याकरण सम्मत हिन्दी सीख पाए। उनकी कक्षा में तीस विद्यार्थी पढ़ते थे, जिनमें से दो तिहाई विवाहित थे। स्वयं उनके भी दो बच्चे थे। एक महिला की तो दो बेटियों की शादी हो गई थी। धुरंधर के सिर पर हर वक्त गरीबी के बादल तने रहते थे। यहां तक कि बस का भाड़ा चुकाकर स्कूल जाना भी उनके लिए मुश्किल होता था। वह तो बस जैसे-तैसे हिन्दी सीख लेना चाहते थे ताकि हिन्दी का शिक्षक बन सकें।
एक बार उन्होंने रोजी रोटी के लिए पुलिस में भी भर्ती होने की कोशिश की लेकिन हुए नहीं। आज रामदेव धुरंधर उपन्यास के रूप में पथरीला सोना के अलावा चेहरों का आदमी, छोटी मछली बड़ी मछली, पूछो इस माटी से, बनते बिगड़ते रिश्ते लिख चुके हैं। उनके विष-मंथन, जन्म की एक भूल आदि कहानी संग्रहों के अलावा कलजुगी धरम, चेहरों के झमेले, पापी स्वर्ग, बंदे आगे भी देख आदि व्यंग्य संग्रह और चेहरे मेरे तुम्हारे, यात्रा साथ-साथ, एक धरती एक आकाश, आते-जाते लोग आदि लघुकथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।
यह भी पढ़ें: अपना काम छोड़कर दिल्ली का यह शख्स अस्पताल के बाहर गरीबों को खिलाता है खाना