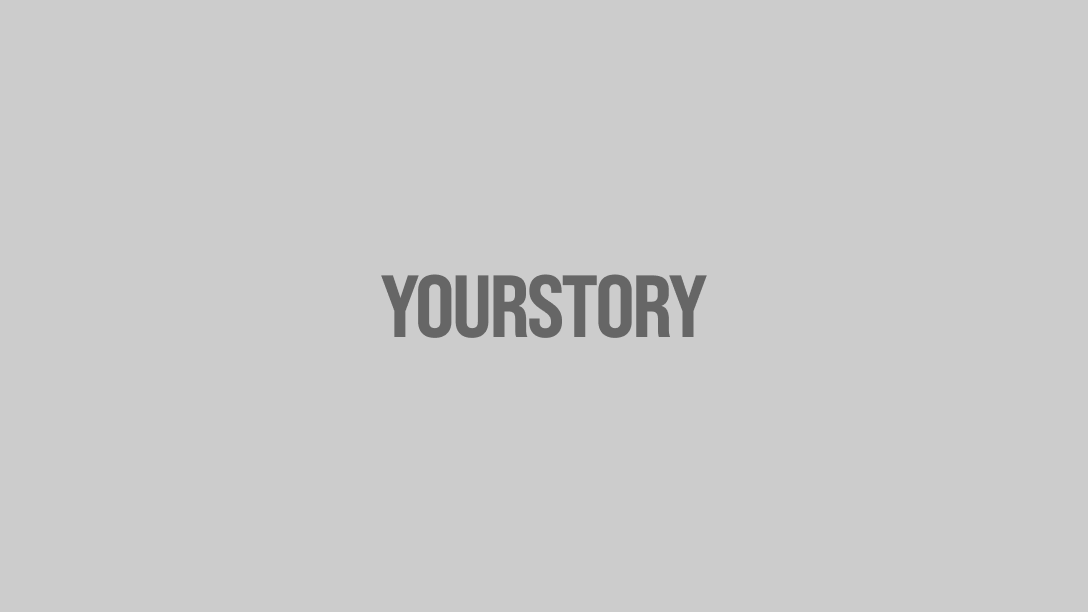प्राथमिकी के तुरंत बाद गिरफ्तारी कितनी सही?
दरअसल प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद लोगों के विरूद्ध उन्हें दोषी मानकर आरोप पत्र प्रेषित करने की प्रवृत्ति तेजी बढ़ी है, जिसके चलते विवेचना का उद्देश्य निरर्थक हो जाता है। दहेज हत्या के मामलों में नाबालिग भाइयों और विवाहित बहनों को भी नामजद कर देना आम है। न्यायपूर्ण निष्पक्ष विवेचना न होने की दशा में ऐसे लोगों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल होता है और वह सभी जेल भेज दिये जाते हैं।

सांकेतिक तस्वीर
राष्ट्रीय पुलिस आयोग का कहना भी है कि देश में 60 फीसदी गिरफ्तारियां अनावश्यक होती हैं जिन पर जेलों का 43.2 प्रतिशत खर्चा होता है। न्यायालय, पुलिस और लोक अभियोजक आपराधिक न्याय प्रक्रिया के आधार स्तम्भ माने जाते हैं। पुलिस अपराधिक मामले में तथ्यान्वेषण तथा साक्ष्य एकत्र करती है और लोक अभियोजक उसे प्रस्तुत कर अभियुक्त को दण्डित करवाने में अहम भूमिका निभाते क्योकि पैरवी वही करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद एवं जगदीश सिंह केहर की खण्ड पीठ ने जघन्य अपराधों में अभियुक्तों की दोषमुक्ति को आपराधिक न्याय प्रशासन की विफलता कहा है। खण्डपीठ ने कहा कि अभियोजन की कमियों के कारण निर्दोष का उत्पीड़न या अपराधी होने के बावजूद अभियोजन की कमियों के कारण किसी की भी दोषमुक्ति समाज की स्थायी सुख-शान्ति के लिए घातक है।
दरअसल प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद लोगों के विरूद्ध उन्हें दोषी मानकर आरोप पत्र प्रेषित करने की प्रवृत्ति तेजी बढ़ी है, जिसके चलते विवेचना का उद्देश्य निरर्थक हो जाता है। दहेज हत्या के मामलों में नाबालिग भाइयों और विवाहित बहनों को भी नामजद कर देना आम है। न्यायपूर्ण निष्पक्ष विवेचना न होने की दशा में ऐसे लोगों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल होता है और वह सभी जेल भेज दिये जाते हैं। राष्ट्रीय पुलिस आयोग का कहना भी है कि देश में 60 फीसदी गिरफ्तारियां अनावश्यक होती हैं जिन पर जेलों का 43.2 प्रतिशत खर्चा होता है। न्यायालय, पुलिस और लोक अभियोजक आपराधिक न्याय प्रक्रिया के आधार स्तम्भ माने जाते हैं। पुलिस अपराधिक मामले में तथ्यान्वेषण तथा साक्ष्य एकत्र करती है और लोक अभियोजक उसे प्रस्तुत कर अभियुक्त को दण्डित करवाने में अहम भूमिका निभाते क्योकि पैरवी वही करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद एवं जगदीश सिंह केहर की खण्ड पीठ ने जघन्य अपराधों में अभियुक्तों की दोषमुक्ति को आपराधिक न्याय प्रशासन की विफलता कहा है। खण्डपीठ ने कहा कि अभियोजन की कमियों के कारण निर्दोष का उत्पीडऩ या अपराधी होने के बावजूद अभियोजन की कमियों के कारण किसी की भी दोषमुक्ति समाज की स्थायी सुख-शान्ति के लिए घातक है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ऐसे लोग जो वर्षों जेल में रहने के बाद जब रिहा होते हैं तो कोई उनका वह समय तथा हुआ सामान वापस नहीं दिला सकता जो उन्होंने निर्दोष होने के बावजूद जेल में रहते हुए गंवाया है। कई बार अपने आपको निर्दोष साबित कराने के लिए उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तक लम्बी कानूनी लड़ायी लड़नी पड़ती है और उसके बाद शुरू होता है, कर्ज शर्म और उत्पीड़न का दर्द। सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार की स्थितियों में निर्दोष नागरिकों के उत्पीडऩ के लिए व्यवस्था को दोषी मानता है। राज्य का दायित्व है कि वह अपने नागरिको के मान-सम्मान और उनकी गरिमा की रक्षा करते हुए और किसी भी दशा में निर्दोष का उत्पीडऩ कदापि न होने दे।
सर्वोच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के प्रत्येक मामले को आपराधिक न्याय प्रशासन की विफलता है और निर्देश दिया कि राज्य सरकार दोष मुक्ति के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए प्रक्रियागत व्यवस्था स्थापित करे। पुलिस और अभियोजन के वरिष्ठ अधिकारियों को इस व्यवस्था के लिए जवाबदेह बनाया जाय। प्रत्येक निर्णय के गुण-दोष पर विचार किया जाय और उसमें इंगित कमियों के लिए जिम्मेदार विवेचक या अभियोजक को चिन्हित किया जाये। कमियों को खोज करके उसके आधार पर विभागीय कार्रवाई करायी जाय। निर्णय में कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रक्रियागत व्यवस्था स्थापित करके सुनिश्चित करायें कि विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष केवल उन्ही मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया जाय जिनमें सजा के लिए समुचित विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध हों।
औपचारिकतावश आरोप पत्र दाखिल न किये जाय बल्कि विवेचना पूरी हो जाने के बाद स्वतन्त्र मस्तिष्क का प्रयोग करके संकलित साक्ष्य की समीक्षा की जाय और यदि उनमें कोई त्रुटि मिले तो बेहिचक उन्हें दूर किया जाय। आवश्यकता प्रतीत हो तो नये सिरे से फिर से साक्ष्य संकलित किये जाय परन्तु किसी भी दशा में अपर्याप्त साक्ष्य होने पर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित नहीं किये जाय। वर्तमान समय में प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अभियोजन अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाती है परन्तु इस बैठक में लोक अभियोजकों द्वारा प्रस्तुत दोष मुक्त आख्या पर चर्चा नहीं होती है। दोष मुक्ति के कारणों को चिन्हित करने और उसके लिए दोषी विवेचक या अभियोजक की जवाबदेही निर्धारित करने की कोई व्यवस्था ही नहीं बनायी गयी है इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च स्तरीय समिति बनाने और उस समिति द्वारा निर्णयों की समीक्षा करने का निर्देश पारित किया है।
यदि सर्वोच्च न्यायालय की मंशा के अनुसार राज्य सरकार अनुपालन सुनिश्चित करायें तो अब जघन्य अपराधों की दोषपूर्ण विवेचना के लिए जिम्मेदार विवेचकों और विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का समुचित पक्ष प्रस्तुत न करने वाले अभियोजकों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई का मार्ग प्रशस्त होगा। विवेचना के उपरान्त विचारण के लिए आरोप पत्र प्रेषित करने के पूर्व उपलब्ध साक्ष्य की एक स्वतन्त्र समिति द्वारा समीक्षा की जायेगी और सुनिश्चित किया जायेगा कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला साक्ष्य अभियुक्त को दोष-सिद्ध करने के पर्याप्त हो। इस प्रक्रिया को अपनाने से किसी निर्दोष को केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हो जाने के कारण विचारण की यातना झेलने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा और अभियोजन को भी अधिकांश मामलों में अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को सिद्ध करना आसान होगा।
दरअसल प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद लोगों के विरूद्ध उन्हें दोषी मानकर आरोप पत्र प्रेषित करने की प्रवृत्ति तेजी बढ़ी है, जिसके चलते विवेचना का उद्देश्य निरर्थक हो जाता है। दहेज हत्या के मामलों में नाबालिग भाइयों और विवाहित बहनों को भी नामजद कर देना आम है। न्यायपूर्ण निष्पक्ष विवेचना न होने की दशा में ऐसे लोगों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल होता है और वह सभी जेल भेज दिये जाते हैं। राष्ट्रीय पुलिस आयोग का कहना भी है कि देश में 60 फीसदी गिरफ्तारियां अनावश्यक होती हैं जिन पर जेलों का 43.2 प्रतिशत खर्चा होता है।
उच्चतम न्यायालय कह चुका है कि जघन्य अपराध के अतिरिक्त गिरफ्तारी को टाला जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट का यह दायित्व है कि वह इन निर्देशों का अनुपालन करायें। किन्तु मजिस्ट्रेट के पर्याप्त सहयोग ने मिलने से पुलिस अनावश्यक गिरफ्तारियां करती है और वकील न तो इनका विरोध करते हैं और न ही मजिस्ट्रेट से इन अनुचित गिरफ्तारियों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 59 के अन्तर्गत बिना जमानत रिहाई की मांग करते हैं। उल्टे इन अनावश्यक गिरफ्तारियों में भी जमानत से इन्कार कर गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश द्वारा अक्सर जेल भेज दिया जाता है। न्यायालयों द्वारा दोषियों के दण्डित होने की सम्भावनायें अत्यन्त क्षीण होने की स्थिति में लोक अभियोजक की भूमिका अग्रिम एवं पश्चातवर्ती जमानत तक ही सीमित हो जाती है।
प्रचलित परम्परानुसार गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत (चाहे उसकी गिरफ्तारी अनावश्यक या अवैध ही क्यों न हो) के लिए भी लोक अभियोजक के निष्क्रिय सहयोग की आवश्यकता होती है अर्थात जमानत आसानी से हो जाय इसके लिए आवश्यक है कि लोक अभियोजक जमानत का विरोध करें। वकीलों में अक्सर चर्चा होती रहती है कि वकील को बोलने के लिए जनता से फीस मिलती है जबकि सरकारी वकील को चुप रहने का रजामन्द करके खरीदा जाता है। ऐसा नहीं है कि यह तथ्य सरकार की जानकारी में नहीं है। क्योंकि सरकार को पता है कि जिस प्रकार राशन डीलर, स्टाम्प विक्रेता आदि सरकार से मिलने वाले नाममात्र के कमीशन पर जीवन यापन नहीं कर सकते और वह अपने जीवनयापन के लिए अन्य अवैध काम भी करते हैं ठीक उसी प्रकार लोक अभियोजकों और सरकारी वकीलों के भी अनैतिक कामों में लिप्त रहने की भरपूर सम्भावनायें मौजूद रहती हैं।
गौरतलब है कि निचले स्तर के मजिस्ट्रेट न्यायालयों में पैरवी करने के लिए अभियोजन संचालन के लिए पूर्णकालिक स्थायी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होते हैं किन्तु न्यायालयों, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में अभियोजन के संचालन के लिए मात्र अंशकालिक और अस्थायी लोक अभियोजक नियुक्त किये जाते हैं। इन लोक अभियोजकों को नाममात्र का पारिश्रमिक देकर उन्हें अपनी आजीविका के लिए अन्य साधनों से गुजारा करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। वर्तमान में लोक अभियोजकों का पारिश्रमिक काफी कम है जबकि सहायक लोक अभियोजकों को पूर्ण वेतन लगभग तीस हजार रुपये दिया जा रहा है।
यह भी एक विरोधाभासी तथ्य है कि सामान्य अपराधों के लिए निचले न्यायालयों में स्थायी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त हैं जबकि ऊपरी न्यायलयों में संगीन अपराधों के परीक्षण और अपील की पैरवी के खातिर अल्प वेतनभोगी अस्थायी लोक अभियोजकों के भरोसे है। यह स्थिति आपराधिक न्याय प्रशासन का मजाक उड़ाती प्रतीत होती है और अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों को दण्डित करने के प्रति सरकार की संजीदगी का एक नमूना मात्र पेश करती है। जाहिर है कि लोक अभियोजक इतने अल्प पारिश्रमिक के कारण पैरवी में न तो कोई रुचि लेते हैं और न ही न्यायालयों द्वारा सामान्यतया अभियुक्तों को दण्डित किया जाता है।
दरअसल लोक अभियोजकों की नियुक्तियां सत्तासीन राजनीतिक दल द्वारा अपनी लाभ-हानि का आंकलन करके देखी जाती हैं और लोक अभियोजक भी अपने नियोक्ता का ध्यान रखते हैं अन्यथा उन्हें किसी भी समय सरकारी कोप-भाजन का शिकार होना पड़ सकता है। कहने का सीधा सा मतलब है कि संगीन जुर्मों के अपराधियों को यदि सरकारी संरक्षण प्राप्त हो तो उस प्रकरण में लोक अभियोजक के माध्यम से पैरवी में लापरवाही बरतकर दण्डित होने से बचा जा सकता है। भारत में राजनीति के अपराधीकरण के लिए यह भी एक प्रमुख कारक है। सरकार जिसे बचाना चाहती है उसके विरुद्ध पैरवी में ढील के निर्देश दे सकती है।
यह व्यवस्था की बदनीयती नहीं तो और क्या है जो साधारण मारपीट के मुकदमों को लडऩे के लिए प्रशिक्षित अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है परन्तु हत्या-डकैती जैसे जघन्य अपराधों के मुकदमों को लडऩे के लिए शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति उनके कार्य-व्यवहार या व्यावसायिक कुशलता को दृष्टिगत रख कर नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं को उपकृत करने की खातिर उनके नेताओं की अनुशंशा पर नियुक्ति की जाती है। नियुक्तियों के लिए सत्तारूढ़ दल के नेताओं की सिफारिश पर होती है, इसलिए आजादी के 66 वर्ष बाद भी व्यावसायिक कुशलता को नियुक्ति का आधार नहीं बनाया गया।
मायावती के मुख्य मन्त्रित्वकाल में सम्पूर्ण प्रदेश में एक साथ सभी शासकीय अधिवक्ताओं को हटा दिया गया था और उनके स्थान पर उन लोगों की नियुक्ति की गयी जो अधिवक्ता के तौर पर साधारण मारपीट का भी मुकदमा अदालत में नहीं लड़े थे। परिणामस्वरूप उनमें से किसी ने भी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान दोष मुक्ति के एक भी मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य अपील दाखिल नहीं की। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को लोक अभियोजकों की नियुक्ति प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन करने होंगे। विधि आयोग ने इस दिशा में कई सुझाव दिये हैं इसके बावजूद राज्य सरकारें राजनीतिक कारणों से उनका पालन करने को तैयार नहीं है।
न्याय प्रशासन की स्वतन्त्रता के लिए अक्सर देश के न्यायविद और उनके समर्थक तर्क देते हैं कि न्याय प्रशासन की पवित्रता के लिए न्यायपालिका की स्वतन्त्रता एवं न्यायाधीशों का निर्भय रहना, एवं उनकी नौकरी में स्थायित्व आवश्यक है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब न्याय प्रशासन के अहम स्तम्भ लोक अभियोजक की सेवा की अनिश्चितता जनित न्याय प्रशासन पर सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव को देश वहन कर सकता है तो न्यायाधीशों की सेवा की अनिश्चितता से देश वास्तव में किस प्रकार कुप्रभावित होगा। अर्थात न्यायाधीशों की सेवा को भी स्थायी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सवाल उठता है कि लोक अभियोजन को दुरुस्त कैसे किया जाये? सबसे पहले तो राज्य सरकारों को समझना होगा कि अपराधी हाईटेक हो गया है। प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य आधारित अभियोजन का युग समाप्त हो चुका है परन्तु विवेचक और अभियोजक मौजूदा समय में भी पुराने तौर तरीकों से काम करते है। केंद्र सरकार द्वारा समुचित धनराशि उपलब्ध कराये जाने के बावजूद राज्य सरकारों ने विवेचक एवं अभियोजक की व्यवसायिक कुशलता बढ़ाने और समय के साथ उसे लय, ताल,कदम बढ़ाने और नये तरीके से ट्रेर्निंग की कोई प्रक्रियागत व्यवस्था नहीं की। जबकि होना यह चाहिये कि विवेचकों और अभियोजकों के नियमित प्रशिक्षण के लिए न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों, उसमे इंगित कमियों और दिन प्रतिदिन के अनुभवों के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाय। इतना ही नहीं हर साल उसकी समीक्षा की जाय। संवेदनशील मामलों की विवेचना के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की बनायी जाय। विवेचना में वैज्ञानिक साधनों और तरीकों को प्रभावी ढंग से लागू करके साक्ष्य खोजने की व्यवस्था बनायी जाय।
ये भी पढ़ें: एक कानून जो प्रधानमंत्री तो बनने देता है लेकिन ग्राम प्रधान नहीं