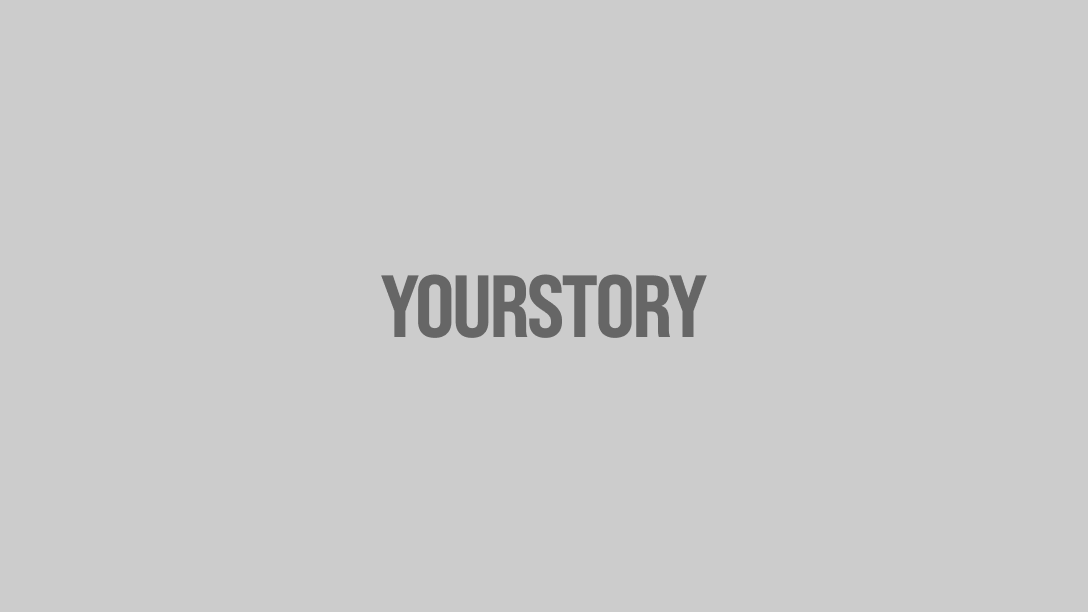आज भी भय और भूख को ललकारते हैं धूमिल
जब तक हमारे मुल्क में, दुनिया में मुफलिसी की लड़ाई है, तब तक कभी न विस्मृत होने वाले कालजयी कवि धूमिल की कविताओं को पढ़ते हुए लगता है, मानो वह हाथ पकड़कर कह रहे हों- 'लो, यह रहा तुम्हारा चेहरा, यह जुलूस के पीछे गिर पड़ा था।' आज महान और निर्भीक सृजनधर्मी धूमिल का जन्मदिन है।
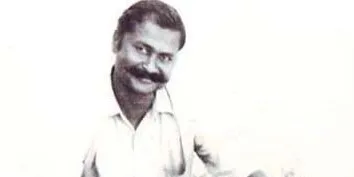
धूमिल
वे कविता के शाश्वत मूल्यों की तलाश करते हैं। वे भाषा, मुहावरों व उक्तियों की सीमाओं से टकराते नजर आते हैं, ताकि कुछ नया दे सकें। इस दृष्टि से वे महत्वपूर्ण हैं कि उन्होंने अपने दौर की कविता को भीड़ से निकाल जनतांत्रिक बनाया।
'एक आदमी
रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है
वह सिर्फ़ रोटी से खेलता है
मैं पूछता हूँ-
'यह तीसरा आदमी कौन है?'
मेरे देश की संसद मौन है।'
जब तक हमारे मुल्क में, दुनिया में मुफलिसी की लड़ाई है, तब तक कभी न विस्मृत होने वाली यह कविता है, हिंदी के कालजयी कवि सुदामा पाण्डेय 'धूमिल' की, जिनका आज (9 नवम्बर) जन्मदिन है। हिन्दी साहित्य की साठोत्तरी कविता के शलाका पुरुष स्वर्गीय सुदामा पाण्डेय धूमिल अपने बागी तेवर, समग्र उष्मा के सहारे संबोधन की मुद्रा में ललकारते दिखते हैं। तत्कालीन परिवेश में अनेक काव्यान्दोलनों का दौर सक्रिय था, परंतु वे किसी के सुर में सुर मिलाने के कायल न थे। उन्होंने तमाम ठगे हुए लोगों को जुबान दी। कालांतर में यही बुलन्द, खनकदार आवाज का कवि जन-जन की जुबान पर छा गया। उनका जन्म 9 नवंबर 1936 को बनारस के खेवली गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की प्राथमिक पाठशाला में हुई। उन्होंने हरहुआ के कूर्मी क्षत्रिय इण्टर कालेज से सन् 1953 ई. में हाईस्कूल की परीक्षा पास की। आगे की पढ़ाई के लिए बनारस पहुंचे तो, मगर अर्थाभाव के चलते उसे जारी न रख सके। फिर क्या, आजीविका की तलाश में वह काशी से कलकत्ता तक भटकते रहे। नौकरी भी मिली तो लाभ कम, मानसिक यंत्रणा ज्यादा। वर्षों का सिरदर्द। अंतत: ब्रेनट्यूमर बनकर मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई।
कवि धूमिल ने सबसे पहली रचना कक्षा सात में लिखी। उनकी प्रारंभिक रचनाएं गीत के रूप में सामने आईं- 'बांसुरी जल गयी', उनके फुटकर शुरुआती गीतों का संकलन है, जो आज उपलब्ध नहीं है। उनकी दो कहानियां 'फिर भी वह जिंदा है' और 'कुसुम दीदी' उनकी मृत्यु के उपरांत 1984 में प्रकाशित हुईं। वैसे उनकी अक्षय कीर्ति की आधार बना 'संसद से सड़क तक' कविता संग्रह, जो सन् 1971 में प्रकाश में आया। भय, भूख, अकाल, सत्तालोलुपता, अकर्मण्यता और अन्तहीन भटकाव को रेखांकित करती, आक्रामकता से भरपूर इस संग्रह की सभी कविताएं अपने में बेजोड़ हैं। पच्चीस कविताओं के इस संग्रह में लगभग सभी रचनाएं तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक परिदृश्य का भी गहराई से परिचय कराती हैं। इस संदर्भ में कवि की समूची राजनैतिक समझ प्रखरता से उभरती है क्योंकि उनकी कविताओं में देहात और शहर, कविकर्म और राजनीति, आस्था और अनास्था, सामाजिकता और असामाजिकता, अहिंसा-हिंसा, ईमानदारी और बेईमानी, जिजीविषा और निराशा आदि प्राय: सभी मानव जीवन से सभ्य-असभ्य अंगों का चित्रण हुआ है। ये सभी चित्रण ठोस सामाजिक यथार्थ के दुर्लभ दस्तावेज हैं। इन कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा अनुभव होता है कि मानो कवि हाथ पकड़कर कह रहा है- लो, यह रहा तुम्हारा चेहरा, यह जुलूस के पीछे गिर पड़ा था।
अकाल दर्शन शीर्षक कविता में कवि प्रश्न करता है- भूख कौन उपजाता है? चतुर आदमी जवाब दिए बगैर बेतहाशा बढती आबादी की ओर इशारा करता है। कवि इस कविता के मार्फत उन लोगों को तलाशता है जो देश के जंगल में भेडिये की तरह लोगों को खा रहे हैं और शोषित उन्हीं की जय-जयकार करने में जुटे हैं। एक दूसरी जोरदार कविता मित्र कवि राजकमल चौधरी के लिए लिख देश का नग्न यथार्थ प्रस्तुत किया है। धूमिल ने राजकमल की हिम्मत के प्रति अगाध श्रद्धा व्यक्त करते हुए लिखा है- वह एक ऐसा आदमी था जिसका मरना/कविता से बाहर नहीं है।
इस कृति की सर्वाधिक चर्चित व असरदार रचना मोचीराम है। इस कविता को धूमिल की प्रतिनिधि कविता माना जाता है। जनपक्षधरता के हिमायती कवि ने प्रतीक व बिम्बों के माध्यम से इसे जन-जन से जोडा है- मेरी निगाह में/ न कोई छोटा है/ न कोई बडा है/.. (वही, पृष्ठ 36) मोचीराम के भीतर एक सजग समाजवेत्ता बैठा है, जो महसूस करता है कि जीने के पीछे एक सार्थक उद्देश्य व तर्क तो होना ही चाहिए। वह जिंदगी को किताबों से नापने का कायल नहीं है।
भाषा की रात भी इस संग्रह की एक प्रखर कविता है। इसमें कवि उन चतुर लोगों को अपना निशाना बनाता है, जो तलवार को कलम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इनकी उदारता में अवसरवाद की गंध है। इसी बहाने वे पूर्व एवं दक्षिण में भाषाई स्तर पर पडी दरार को भी उद्घाटित करते हैं- चंद चालाक लोगों ने.. बहस के लिए/ भूख की जगह/ भाषा को रख दिया है। धूमिल की अधिकांश कविताओं में कुछ ऐसे शब्द हैं, जो अक्सर मिल जाते हैं जैसे- जंगल, भूख, विदेशी मुद्रा, अमीन, लाल-हरी झण्डियां, फाइलें, विज्ञापन, वारण्ट आदि। ये सीधे तौर पर कवि के राजनीतिक-सामाजिक विमर्श की ओर संकेत करते हैं। धूमिल अपने परिवेश और जटिल परिस्थितियों के प्रति अत्यन्त सक्रिय हैं। वे कविता के शाश्वत मूल्यों की तलाश करते हैं। वे भाषा, मुहावरों व उक्तियों की सीमाओं से टकराते नजर आते हैं, ताकि कुछ नया दे सकें। इस दृष्टि से वे महत्वपूर्ण हैं कि उन्होंने अपने दौर की कविता को भीड़ से निकाल जनतांत्रिक बनाया। उसका रुख ही बदल दिया। जनतंत्र का सूर्योदय, मुनासिब कार्यवाई, बारिश में भीगकर और सर्वाधिक लम्बी कविता पटकथा इस दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। प्रस्तुत है- 'जनतन्त्र के सूर्योदय में' कविता-
रक्तपात –
कहीं नहीं होगा
सिर्फ़, एक पत्ती टूटेगी!
एक कन्धा झुक जायेगा!
फड़कती भुजाओं और सिसकती हुई आँखों को
एक साथ लाल फीतों में लपेटकर
वे रख देंगे
काले दराज़ों के निश्चल एकान्त में
जहाँ रात में
संविधान की धाराएँ
नाराज़ आदमी की परछाईं को
देश के नक्शे में
बदल देती है
पूरे आकाश को
दो हिस्सों में काटती हुई
एक गूँगी परछाईं गुज़रेगी
दीवारों पर खड़खड़ाते रहेंगे
हवाई हमलों से सुरक्षा के इश्तहार
यातायात को
रास्ता देती हुई जलती रहेंगी
चौरस्तों की बस्तियाँ
सड़क के पिछले हिस्से में
छाया रहेगा
पीला अन्धकार
शहर की समूची
पशुता के खिलाफ़
गलियों में नंगी घूमती हुई
पागल औरत के 'गाभिन पेट' की तरह
सड़क के पिछले हिस्से में
छाया रहेगा पीला अन्धकार
और तुम
महसूसते रहोगे कि ज़रूरतों के
हर मोर्चे पर
तुम्हारा शक
एक की नींद और
दूसरे की नफ़रत से
लड़ रहा है
अपराधियों के झुण्ड में शरीक होकर
अपनी आवाज़ का चेहरा टटोलने के लिए
कविता में
अब कोई शब्द छोटा नहीं पड़ रहा है :
लेकिन तुम चुप रहोगे;
तुम चुप रहोगे और लज्जा के
उस गूंगेपन-से सहोगे –
यह जानकर कि तुम्हारी मातृभाषा
उस महरी की तरह है, जो
महाजन के साथ रात-भर
सोने के लिए
एक साड़ी पर राज़ी है
सिर कटे मुर्गे की तरह फड़कते हुए
जनतन्त्र में
सुबह –
सिर्फ़ चमकते हुए रंगों की चालबाज़ी है
और यह जानकर भी, तुम चुप रहोगे
या शायद, वापसी के लिए पहल करनेवाले –
आदमी की तलाश में
एक बार फिर
तुम लौट जाना चाहोगे मुर्दा इतिहास में
मगर तभी –
य़ादों पर पर्दा डालती हुई सबेरे की
फिरंगी हवा बहने लगेगी
अख़बारों की धूल और
वनस्पतियों के हरे मुहावरे
तुम्हें तसल्ली देंगे
और जलते हुए जनतन्त्र के सूर्योदय में
शरीक़ होने के लिए
तुम, चुपचाप, अपनी दिनचर्या का
पिछला दरवाज़ा खोलकर
बाहर आ जाओगे
जहाँ घास की नोक पर
थरथराती हुई ओस की एक बूंद
झड़ पड़ने के लिए
तुम्हारी सहमति का इन्तज़ार
कर रही है।
'कल सुनना मुझे' संग्रह सन् 77 में धूमिल के मृत्योपरान्त प्रकाश में आया। वे हमेशा आत्म सम्मोहन और लेखकीय दादागीरी के खिलाफ रहे। किसी भी कविता को वे पहले सूक्तियों में लिखते थे। असल में बहुत ही अव्यवस्थित और बिखरा-बिखरा उनका कवि कर्म उन्हें अन्य साहित्यकारों से अलग करता है। इसकी पृष्ठभूमि में उनका गंवई जीवन था। वे घर-घर की समस्याओं, मुकदमेबाजी, पारिवारिक असंगतियों, अंधविश्वास और पिछडेपन का दंश झेलते हुए कविता-रचना के लिए समय निकाल लेते। वे शहर की चतुराई, बेहयाई, छल प्रपंच से परिचित हैं। पूंजीवादी बाजार व्यवस्था को वे अकेले चुनौती देते हैं। वे पहले ऐसे कवि हैं जो आत्महीनता के खिलाफ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, कविता के द्वारा जरूरी हस्तक्षेप करते हैं। उनकी कविता जिंदगी के ताप से भरती चलती है और ठहरे हुए आदमी को हरकत में लाकर ही दम लेती है। सन् 1984 में धूमिल की तीसरी और अंतिम अनूठी काव्यकृति सुदामा पाण्डेय का प्रजातंत्र आने पर पर्याप्त ख्याति अर्जित कर चुकी थी। यह संग्रह तत्कालीन साम्राज्यवादी ताकतों को बेनकाब करती है। कवि एक ठोस सैद्धांतिक धरातल पर खडा होकर अव्यवस्था और अमानवीयता के प्रति मुखर हो उठता है। इस अव्यवस्था की जडों को उखाड फेंकने के लिए वह विचारधारा के माध्यम से संघर्ष करता है-
न मैं पेट हूं
न दिवार हूं
न पीठ हूं
अब मैं विचार हूं।
धूमिल तमाम तरह की विद्रूपताओं को खुलकर कहते और लिखते रहे। इसीलिए उन पर आरोप है कि विशेष रूप से नारी के प्रति वितृष्णा से भरा है। ध्यान रहे- यह उनकी सभी कविताओं के साथ जोड़कर न देखें तो न्याय होगा। मां और पत्नी के प्रति उनका आत्मीय संबंध लाजवाब है। सच तो यह है कि उन्होंने अतिशय यथार्थ सामने रखकर उन बातों से अश्लीलता के प्रति वितृष्णा पैदा करने की कोशिश भर की है। इस संबंध में विद्यानिवास मिश्र लिखते हैं- 'धूमिल के काव्य में काम नहीं है बल्कि कामुकता के प्रति गहरी वितृष्णा है। वह पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र की तरह गरिमा के लिए ही कुछ तीखा होना चाहता है। धूमिल के काव्य की जांच इसलिए धूमिल की वास्तविक चिंता की दृष्टि से की जानी शेष है, भाषा के तेवर की, विचार की तीक्ष्णता की चर्चा तो बहुत हो चुकी है।' कवि धूमिल का शिल्प-विधान और भाषा अपने समकालीन सरोकारों, गंवई सुगंध, ईमानदार व्यक्ति की बगैर लपछप की एक अनूठी झलक है। उनकी नजर में कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। वे मानते हैं- एक सही कविता पहले एक सार्थक व्यक्तव्य होती है। यह भी सच है, कि वे भाषा का भ्रम तोडना चाहते हैं। वे जनता की यातना और दुख से उभरी तेजस्वी भाषा में कविताई करना पसंद करते हैं। वे कहते हैं- आज महत्व शिल्प का नहीं, कथ्य का है, सवाल यह नहीं कि आपने किस तरह कहा है, सवाल यह है कि आपने क्या कहा है-
करछुल...
बटलोही से बतियाती है और चिमटा
तवे से मचलता है
चूल्हा कुछ नहीं बोलता
चुपचाप जलता है और जलता रहता है
औरत...
गवें गवें उठती है...गगरी में
हाथ डालती है
फिर एक पोटली खोलती है।
उसे कठवत में झाड़ती है
लेकिन कठवत का पेट भरता ही नहीं
पतरमुही (पैथन तक नहीं छोड़ती)
सरर फरर बोलती है और बोलती रहती है
बच्चे आँगन में...
आंगड़बांगड़ खेलते हैं
घोड़ा-हाथी खेलते हैं
चोर-साव खेलते हैं
राजा-रानी खेलते हैं और खेलते रहते हैं
चौके में खोई हुई औरत के हाथ
कुछ नहीं देखते
वे केवल रोटी बेलते हैं और बेलते रहते हैं
एक छोटा-सा जोड़-भाग
गश खाती हुई आग के साथ
चलता है और चलता रहता है
बड़कू को एक
छोटकू को आधा
परबती... बालकिशुन आधे में आधा
कुछ रोटी छै
और तभी मुँह दुब्बर
दरबे में आता है... 'खाना तैयार है?'
उसके आगे थाली आती है
कुल रोटी तीन
खाने से पहले मुँह दुब्बर
पेटभर
पानी पीता है और लजाता है
कुल रोटी तीन
पहले उसे थाली खाती है
फिर वह रोटी खाता है
और अब...
पौने दस बजे हैं...
कमरे में हर चीज़
एक रटी हुई रोज़मर्रा धुन
दुहराने लगती है
वक्त घड़ी से निकल कर
अंगुली पर आ जाता है और जूता
पैरों में, एक दंत टूटी कंघी
बालों में गाने लगती है
दो आँखें दरवाज़ा खोलती हैं
दो बच्चे टा टा कहते हैं
एक फटेहाल क्लफ कालर...
टाँगों में अकड़ भरता है
और खटर पटर एक ढड्ढा साइकिल
लगभग भागते हुए चेहरे के साथ
दफ्तर जाने लगती है
सहसा चौरस्ते पर जली लाल बत्ती जब
एक दर्द हौले से हिरदै को हूल गया
'ऐसी क्या हड़बड़ी कि जल्दी में पत्नी को चूमना...
देखो, फिर भूल गया।
धूमिल की भाषा का संबोधनात्मक प्रयोग भी उन्हें तमाम समकालीन मुलम्मेदार व पाण्डित्य-प्रदर्शन-प्रिय कवियों से अलग व एक विशिष्ट पहचान देता है। उनकी कविता नये विम्ब विधान व नये संदर्भो में जनता के संघर्ष के स्वर में स्वर मिलाती है। इस दृष्टि से उनकी काव्यभाषा सामाजिक संरचना के औचित्य को चुनौती देती है। उनके काव्य बिंब अपने परवर्ती कवियों से पृथक हैं। वे अपनी प्रकृति और प्रस्तुति में अद्भुत हैं-धूप मां की गोद सी गर्म थी। कहकर कवि मां की महिमा को सिर माथे स्वीकारता है। छंदविधान की दृष्टि से उनकी लगभग सभी कविताएं गद्यात्मक लय की ओर झुकी हुई हैं। कविता की एकरसता और लंबाई तोडने के उद्देश्य से वे पंक्तियों को छोटा-बडा करते हैं और तुकों द्वारा तालमेल एवं लय स्थापित करते हैं। हिंदी कविता को नए तेवर देने वाले इस जनकवि का योगदान चिरस्मरणीय है और रहेगा। 'धूमिल की अन्तिम कविता' -
शब्द किस तरह
कविता बनते हैं
इसे देखो
अक्षरों के बीच गिरे हुए
आदमी को पढ़ो
क्या तुमने सुना कि यह
लोहे की आवाज़ है या
मिट्टी में गिरे हुए ख़ून
का रंग।
लोहे का स्वाद
लोहार से मत पूछो
घोड़े से पूछो
जिसके मुंह में लगाम है।
यह भी पढ़ें: सुजाता को पहली ही किताब पर अमेरिका में लाखों का सम्मान