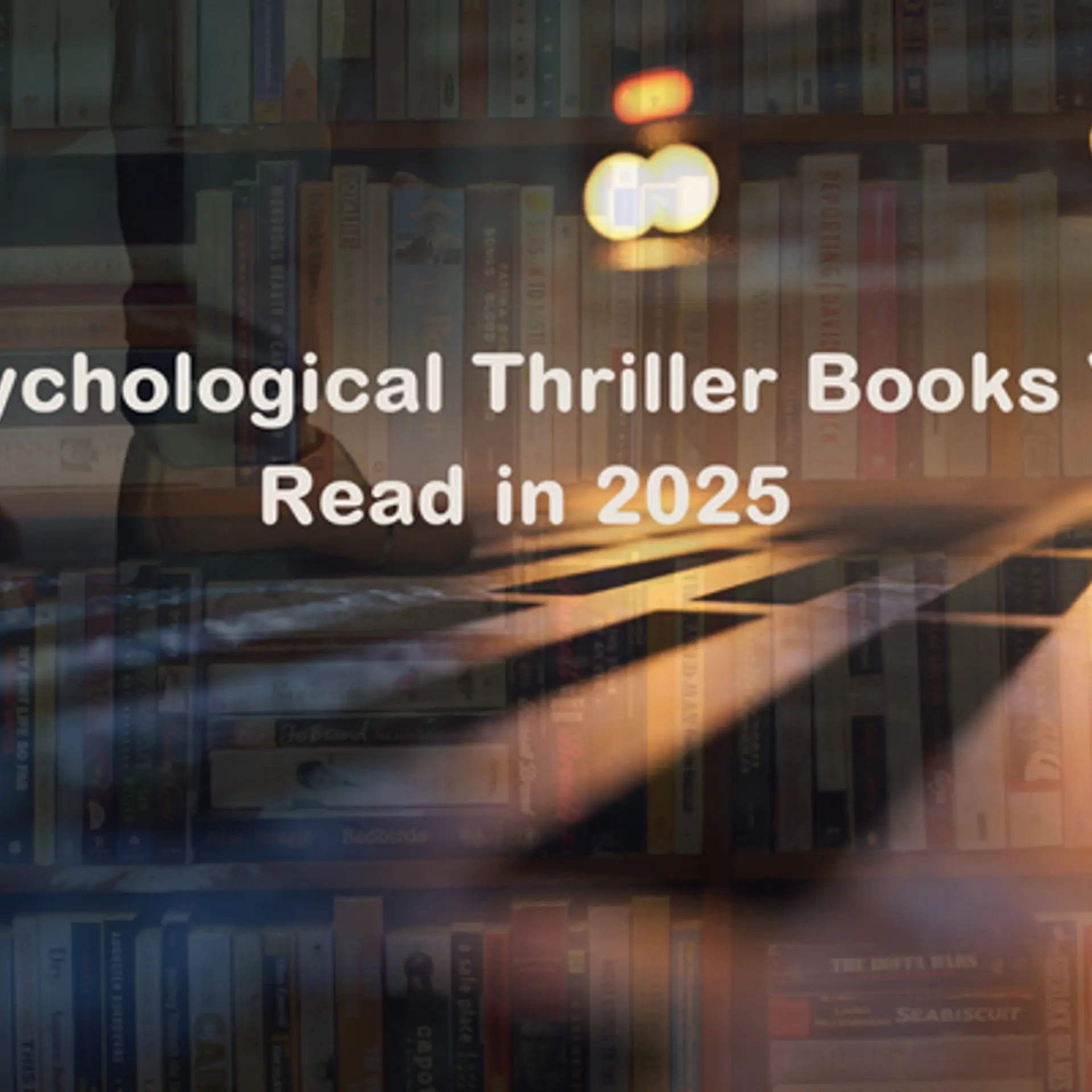होगा किसी दीवार के साए में पड़ा ‘मीर’
मीर कल, आज और कल...
'मीर' के ज़माने को लगभग 200 वर्ष हो गये। ज़बान बदल गयी, अभिव्यक्ति का ढंग बदल गया, काव्य-रुचि बदल गयी किन्तु 'मीर' जैसे अपने ज़माने में लोकप्रिय थे वैसे ही आज भी हैं।

मीर तकी मीर का रेखांकन
दरअसल 'मीर' की स्थायी सफलता का रहस्य यही है कि उन्होंने अपनी दुख की संवेदना को इतना मुखर कर दिया था कि उनके सीधे-सादे शब्द भी हर ज़माने में बड़े-बड़े काव्य-मर्मज्ञों को प्रभावित करते रहे हैं।
ख़ुदा-ए-सुखन मोहम्मद तकी उर्फ मीर तकी 'मीर' उर्दू एवं फ़ारसी भाषा के महान शायर थे। वह आज ही के दिन इस दुनिया-ए-फानी से कूच कर गए थे। उनको शायरी का ख़ुदा कहा जाता है। उन्हें उर्दू के उस चलन के लिए याद किया जाता है, जिसमें फ़ारसी और हिन्दुस्तानी का सुंदर सम्मिश्रण और सामंजस्य हो - होगा किसी दीवार के साए में पड़ा 'मीर', क्या काम मोहब्बत से उस आराम-तलब को।
मीर का जन्म आगरा में हुआ और इंतकाल लखनऊ में। बचपन पिता की देख-रेख में गुज़रा। लखनऊ ही में 'मीर' ने अपना जीवन चरित्र 'ज़िक्रे-मीर' लिखा। उस समय उनकी अवस्था लगभग साठ वर्ष की थी। इसमें उन्होंने अपने निजी जीवन की घटनाओं के साथ ही अपने ज़माने की राजनीतिक उथल-पुथल (बल्कि अराजकता की स्थिति) का विस्तार-पूर्वक उल्लेख किया है। विभिन्न दरबारों और रईसों से सम्बन्धित रहने और सारी राजनीतिक हलचलों को अपनी आंखों से देखने के कारण उनके लिए यह संभव भी हो सका। पिता की मौत के बाद वह दिल्ली आ गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह वहाँ ही दरबारी शायर करने लगे। अहमद शाह अब्दाली के हमलों की तबाही के बाद वह लखनऊ गए और जिंदगी के आखिर तक वहीं के होकर रहे। उन्होंने ने कुल 13585 शेर लिखे। मीर को एक बार ग़ालिब ने जब किसी फकीर से मीर की एक नज्म सुनी तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकला-
रेख्ते के तुम ही नहीं हो उस्ताद ग़ालिब, कहते हैं पिछले ज़माने में कोई मीर भी था
अहमद शाह अब्दाली और नादिरशाह के हमलों से परेशान दिल्ली को मीर तक़ी मीर ने अपनी आँखों से देखा था। उस त्रासदी की तस्वीर उनकी रचनाओं में साया है। अपनी ग़ज़लों के बारे में मीर ने कहा था-
हमको शायर न कहो मीर कि साहिब हमने, दर्दो ग़म कितने किए जमा तो दीवान किया
उस समय शाही दरबार में फ़ारसी शायरी को अधिक महत्व दिया जाता था। मीर तक़ी मीर को उर्दू में शेर कहने का प्रोत्साहन अमरोहा के सैयद सआदत अली ने दिया। २५-२६ साल की उम्र तक ये एक दीवाने शायर के रूप में ख्यात हो गए थे। १७४८ में इन्हें मालवा के सूबेदार के बेटे का मुसाहिब बना दिया गया। मीर कहते हैं -
हम जानते तो इश्क न करते किसी के साथ, ले जाते दिल को खाक में इस आरजू के साथ
मजरूह अपनी छाती को बखिया किया बहुत, सीना गठा है 'मीर' हमारा रफू के साथ।
मीर की ग़ज़लों के कुल छह दीवान हैं। इनमें से कई शेर ऐसे हैं, जो मीर के हैं या नहीं, इस पर बड़ा झमेला है। इसके अलावा कई शेर या कसीदे ऐसे हैं, जो किसी और के संकलन में हैं पर ऐसा मानने वालों की कमी नहीं कि वे मीर के हैं। इसके अलावा कुल्लियात-ए-मीर में दर्जनों मसनवियाँ (स्तुतिगान), क़सीदे, वासोख़्त और मर्सिये संकलित हैं। मीर अपनी कामयाबियों को कुछ इस अदा से नवाजते हैं -
मिरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में, तमाम उम्र मैं नाकामियों से काम लिया
उर्दू के महान शायरों में शुमार 'मीर तक़ी मीर' को ऐसे ही नहीं 'ख़ुदा-ए-सुख़न' (शायरी का ख़ुदा) कहा जाता है। 'मीर' ने तो शायद यह शेर कवि सुलभ आत्माभिमान की दृष्टि से कहा हो किन्तु यह बात पूर्णतः सच निकली है। 'मीर' के ज़माने को लगभग 200 वर्ष हो गये। ज़बान बदल गयी, अभिव्यक्ति का ढंग बदल गया, काव्य-रुचि बदल गयी किन्तु 'मीर' जैसे अपने ज़माने में लोकप्रिय थे वैसे ही आज भी हैं। कोई ज़माना ऐसा नहीं गुजरा जब कि उस्तादों ने 'मीर' का लोहा न माना हो। उनके प्रतिद्वंद्वी 'सौदा' ने भी, जो निन्दात्मक काव्य के बादशाह समझे जाते हैं और जिनकी कभी-कभी 'मीर' से शायराना चोटें चल जाती थीं, 'मीर' की खुले शब्दों में प्रशंसा की है -
सौदा' तू इस ज़मीं से ग़ज़ल-दर-ग़ज़ल ही लिख, होना है तुझको 'मीर' से उत्साद की तरफ़।।
उर्दू भाषा की सबसे अधिक साज-संवार करने वाले उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लखनवी उस्ताद 'नासिख़' का मिसरा है - आप बे-बहरा है जो मोतक़दे-'मीर' नहीं। 'ग़ालिब' ने भी 'नासिख' का हवाला देकर उनके विचार की पुष्टि की है - ग़ालिब' अपना को अक़ीदा है ब-क़ौले-नासिख़'। आप बे-बहरा है जो मोतक़दे-'मीर' नहीं। प्रकाश पंडित लिखते हैं कि दरअसल 'मीर' की स्थायी सफलता का रहस्य यही है कि उन्होंने अपनी दुख की संवेदना को इतना मुखर कर दिया था कि उनके सीधे-सादे शब्द भी हर ज़माने में बड़े-बड़े काव्य-मर्मज्ञों को प्रभावित करते रहे हैं। भाग्य ने उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके समय की सामाजिक परिस्थतियों को स्थिरता और आराम-चैन से इतना अलग कर दिया था कि 'मीर' का हृदय एक टूटा हुआ खंडहर बन गया और उसमें से दर्दों-गम की ऐसी तानें निकली जिन्होंने 'मीर' को कविता के क्षेत्र में अमरत्व प्रदान कर दिया-
पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख़्तों को लोग, मुद्दत रहेंगी याद ये बातें हमारियां।
मीर जिन दिनो लखनऊ में रहते थे, उनके घर पर मुशायरा हुआ करता था। उसमें एक दिन 'ज़ुर्रत' ने, जो नयी उठान के चंचलता-प्रिय कवि थे, अपनी ग़ज़ल पढ़ी जिसकी तत्कालीन रुचि के मुताबिक़ खूब तारीफ़ हुई। 'मीर' चुपचाप बैठे रहे। 'ज़ुर्रत' को मुशायरे में मिली प्रशंसा काफ़ी न मालूम हुई तो 'मीर' साहब के पास आकर बैठ गये और अपनी ग़ज़ल के बारे में उनकी राय जाननी चाही। 'मीर' साहब ने टालमटोल करनी चाही, लेकिन शामत के मारे 'ज़ुर्रत' पीछे पड़े गये। 'मीर' साहब त्योरी चढ़ा कर बोले, कैफ़ीयत इसकी यह है कि तुम शेर तो कहना नहीं जानते हो, अपनी चूमाचाटी कह लिया करो-
राह-ए-दूर-ए-इश्क़ में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या
'मीर' शायरी को सिर्फ़ मन-बहलाव की चीज़ नहीं समझते थे, बल्कि उसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण बल्कि सबसे महत्वपूर्ण अंग मानते थे और दूसरों से भी ऐसी ही आशा करते थे। मीर की क़िस्मत में चैन से रहना न बदा था। नादिरशाह ने दिल्ली पर हमला किया तो नवाब समसामुद्दौला इसमें मारे गये। मीर सहारा टूटने पर आगरा पहुंचे लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दिल्ली पहुंचे और अपने सौतेले भाई के मामा ख़ान आरजू के पास रहने लगे। कुछ दिन उनसे कुछ पढ़ा-सीखा। ख़ान आरजू उस ज़माने के शीर्ष शायरों में थे लेकिन फिर वे उनसे नाराज़ हो गये। मीर का कहना था कि सौतेले भाई की शिकायत पर खान आरजू उनसे बिगड़े थे। कुछ लोग इसका कारण यह बताते है कि वे खान आरजू की पुत्री से प्रेम करने लगे थे। यह प्रेम इतना बढ़ा कि उन्होंने सबसे मिलना-ज़ुलना छोड़ दिया और एक कोठरी में पड़े रहते -
देख तो दिल कि जां से उठता है ये धुआं सा कहां से उठता है
गोर किस दिल-जले की है ये फलक शोला इक सुबह यां से उठता है
नाला सर खेंचता है जब मेरा शोर एक आसमान से उठता है
लड़ती है उस की चश्म-ऐ-शोख जहां इक आशोब वां से उठता है
सुध ले घर की भी शोला-ऐ-आवाज़, दूद कुछ आशियां से उठता है
बैठने कौन दे है फिर उस को, जो तेरे आस्तां से उठता है
यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है
इश्क इक 'मीर' भारी पत्थर है, बोझ कब नातावां से उठता है
यह भी पढ़ें: कुंवर नारायण फिल्म की तरह टुकड़ों में लिखते हैं कविता