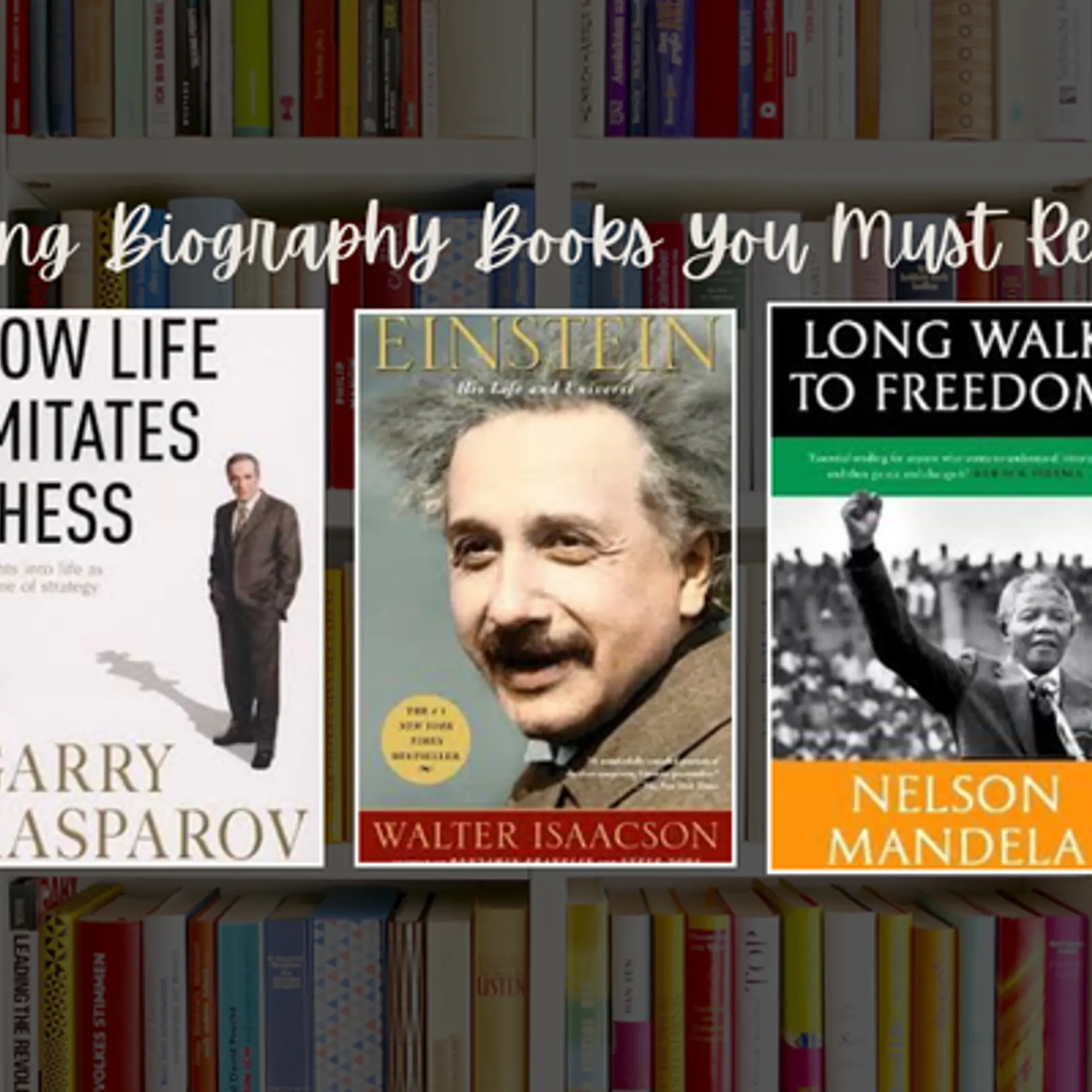सतत विकास लक्ष्य-7 क्या है? कैसे क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी को देगा बढ़ावा?
SDG के 17 लक्ष्यों में 7वां सतत विकास लक्ष्य (SDG-7 या वैश्विक लक्ष्य-7) सभी के लिए अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी से संबंधित है. इसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है.
सतत विकास लक्ष्य (SDG) या ‘2030 एजेंडा’ बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए सभी से कार्रवाई का आह्वान करता है. वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था. 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग हैं.
17 एसडीजी मानते हैं कि एक क्षेत्र में कार्रवाई से दूसरे क्षेत्र में परिणाम प्रभावित होंगे, और यह कि विकास को अवश्य ही प्रभावित होना चाहिए. सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता को संतुलित करें. एक प्रणालीगत सोच दृष्टिकोण वैश्विक स्थिरता के लिए आधार है.
SDG के 17 लक्ष्यों में 7वां सतत विकास लक्ष्य (SDG-7 या वैश्विक लक्ष्य-7) सभी के लिए अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी से संबंधित है. इसका उद्देश्य सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है. लोगों की भलाई के साथ-साथ आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए ऊर्जा तक पहुंच एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है.
इस लक्ष्य के तहत 5 टारगेट निर्धारित हैं, जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है. इन टारगेट को मापने के लिए 6 संकेतक हैं.
1. आधुनिक ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच
2. नवीकरणीय ऊर्जा में वैश्विक अनुपात को बढ़ाना
3. ऊर्जा दक्षता में दोगुना सुधार
4. क्लीन एनर्जी में रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इंवेस्टमेंट को बढ़ावा देना
5. विकासशील देशों के लिए एनर्जी सर्विसेज का विस्तार करना और उन्हें बढ़ावा देना
घरेलू वायु प्रदूषण से सालाना 15 लाख मौतें
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, आज भी 2.4 अरब लोग (लगभग दुनिया की 40 फीसदी आबादी) खाने पकाने के लिए पारंपरिक जैविक ईंधन पर निर्भर है. इस तरह के लो क्वालिटी के ईंधन घर के अंदर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं.
यहां तक कि एनर्जी की पहुंच और आर्थिक विकास को बढ़ाने के बाद भी घरेलू वायु प्रदूषण से होने वाली सालाना मौतें 15 लाख से अधिक रहेंगी. यह संख्या मलेरिया और टीबी से होने वाली सालाना मौतों से भी अधिक है.
20 फीसदी आबादी तक बिजली की पहुंच नहीं
साल 2010 में 1.2 अरब लोगों के पास बिजली की पहुंच नहीं थी. साल 2020 में यह संख्या 73.3 लाख थी. आज भी दुनिया की 20 फीसदी आबादी तक बिजली की पहुंच नहीं है. इसके अलावा एक बड़ी आबादी को लगातार बिजली के संकट से जूझना पड़ता है. वहीं, 2030 में भी बिजली के अभाव में जीने वाले लोगों की संख्या 67.9 लाख तक रहने का अनुमान है.
रिन्यूएबल एनर्जी को नहीं मिल रहा बढ़ावा
रिन्यूएबल एनर्जी की कुल खपत साल 2010 से 2019 के बीच एक चौथाई बढ़ी है जबकि कुल ऊर्जा में रिन्यूएबल एनर्जी की कुल हिस्सेदारी 2019 में केवल 17.7 फीसदी थी.
रिन्यूएबल एनर्जी के लिए विकासशील देशों को मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहायता में भी लगातार पिछले दो सालों में गिरावट आई है. साल 2017 में यह जहां 20 खरब रुपये थी तो वहीं, 2018 में यह घटकर 12 खरब रुपया रह गया. 2019 में यह घटकर 9 खरब रुपये तक पहुंच गया.
2012 में रुक गई थी भारत की अर्थव्यवस्था
साल 2012 में, बड़े पैमाने पर देशव्यापी ब्लैकआउट ने भारत को प्रभावित किया था. इसने लगभग 70 लाख लोगों को प्रभावित किया, परिवहन और संचार प्रणालियों को पंगु बना दिया और कई लोगों की मौतें हुईं.
यह आपदा न केवल सप्लाई से जुड़े मुद्दों के कारण हुई, बल्कि कुप्रबंधन और एक अविकसित ऊर्जा के बुनियादी ढांचे के कारण भी हुई. इस प्रकार, बुनियादी आर्थिक गतिविधि एक स्थिर आपूर्ति, मजबूत शासन और एक कुशल और स्थिर वितरण प्रणाली पर निर्भर करती है. ऊर्जा विश्वसनीयता के कई सामाजिक आर्थिक आयाम हैं.
Edited by Vishal Jaiswal